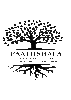अध्याय 10: मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार
- परिचय
- मानव नेत्र
- मुख्य भाग और उनके कार्य
- समंजन क्षमता
- निकट बिंदु
- दूर बिंदु
- दृष्टि दोष और उनका संशोधन
- निकट दृष्टि दोष (Myopia)
- दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia)
- जरादूरदृष्टिता (Presbyopia)
- अबिंदुकता (Astigmatism)
- प्रकाश का अपवर्तन – कांच के प्रिज्म से अपवर्तन
- विचलन कोण
- प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
- स्पेक्ट्रम
- वायुमंडलीय अपवर्तन
- तारों का टिमटिमाना
- अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त
- आभासी चपटा आकार
- प्रकाश का प्रकीर्णन
- आकाश का नीला रंग
- सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग
- खतरे के सिग्नल का लाल रंग
- अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है
- सारांश
- अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु
परिचय:
यह अध्याय हमें मानव नेत्र की संरचना, उसके कार्य करने के तरीके और प्रकाश के अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाओं के कारण हमारे आसपास दिखाई देने वाले रंगबिरंगे संसार के बारे में बताता है। यह नोट्स NCERT की पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री पर आधारित हैं ताकि आपको विषय को आसानी से समझने में मदद मिल सके।
मुख्य विषय:
- मानव नेत्र (The Human Eye):
- मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है। यह कैमरे की तरह कार्य करता है।
- मुख्य भाग और उनके कार्य:
- कॉर्निया (Cornea): यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी, उभरी हुई झिल्ली है। यह प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है और अधिकांश अपवर्तन (प्रकाश का मुड़ना) यहीं पर होता है।
- आइरिस (Iris) या परितारिका: यह कॉर्निया के पीछे स्थित एक रंगीन पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। आइरिस का रंग व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है।
- पुतली (Pupil) या नेत्र तारा: यह आइरिस के केंद्र में स्थित एक छोटा छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में फैल जाती है।
- नेत्र लेंस (Eye Lens): यह आइरिस के पीछे स्थित एक पारदर्शी, द्विउत्तल (biconvex) लेंस है। यह लचीला होता है और इसकी फोकस दूरी को सिलिअरी मांसपेशियों (Ciliary Muscles) द्वारा समायोजित किया जा सकता है ताकि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके।
- सिलिअरी मांसपेशियाँ (Ciliary Muscles): ये नेत्र लेंस से जुड़ी मांसपेशियाँ हैं जो लेंस की वक्रता को बदलकर उसकी फोकस दूरी को समायोजित करती हैं।
- रेटिना (Retina) या दृष्टिपटल: यह नेत्र के पीछे की आंतरिक परत है जो प्रकाश-संवेदी कोशिकाओं (प्रकाशग्राही – Photoreceptors) से बनी होती है। यहाँ वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दो प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएँ होती हैं:
- शंकु (Cones): ये तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं और हमें रंगों को देखने में मदद करते हैं। तीन प्रकार के शंकु होते हैं जो लाल, हरे और नीले रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- शलाकाएँ (Rods): ये मंद रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं और हमें काली और सफेद वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं।
- दृक् तंत्रिका (Optic Nerve): यह तंत्रिका रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य सूचनाओं को ले जाती है। रेटिना पर वह बिंदु जहाँ से दृक् तंत्रिका निकलती है, अंध बिंदु (Blind Spot) कहलाता है क्योंकि इस बिंदु पर कोई प्रकाशग्राही कोशिकाएँ नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ कोई दृष्टि नहीं होती।
- जलीय द्रव (Aqueous Humor): यह कॉर्निया और लेंस के बीच भरा हुआ एक पतला, जलीय द्रव है जो नेत्र को पोषण प्रदान करता है और आकार बनाए रखने में मदद करता है।
- काचाभ द्रव (Vitreous Humor): यह लेंस और रेटिना के बीच भरा हुआ एक गाढ़ा, जेली जैसा द्रव है जो नेत्र को आकार बनाए रखने में मदद करता है।
- समंजन क्षमता (Power of Accommodation):
- नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से रेटिना पर फोकस कर सकता है, समंजन क्षमता कहलाती है।
- जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, तो सिलिअरी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है।
- जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं, तो सिलिअरी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है।
- निकट बिंदु (Near Point) या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी: वह निकटतम बिंदु जिस पर कोई सामान्य नेत्र बिना किसी तनाव के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। सामान्य वयस्क नेत्र के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है।
- दूर बिंदु (Far Point): वह दूरतम बिंदु जिसे कोई सामान्य नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है। सामान्य नेत्र के लिए यह बिंदु अनंत होता है।
- दृष्टि दोष और उनका संशोधन (Defects of Vision and Their Correction):
- कुछ कारणों से नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है, जिसके कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ सामान्य दृष्टि दोष निम्नलिखित हैं:
- निकट दृष्टि दोष (Myopia) या लघुदृष्टि: इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि:
- नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है।
- नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है।
- संशोधन: इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस (concave lens) का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित (diverge) करता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।
- दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) या दीर्घदृष्टि: इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि:
- नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है।
- नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है।
- संशोधन: इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस (convex lens) का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित (converge) करता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।
- जरादूरदृष्टिता (Presbyopia): यह दोष उम्र बढ़ने के कारण होता है। सिलिअरी मांसपेशियों की कमजोरी और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है। इसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है।
- संशोधन: इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस (bifocal lenses) का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग दूर की दृष्टि के लिए अवतल लेंस और निचला भाग पास की दृष्टि के लिए उत्तल लेंस होता है। आजकल प्रोग्रेसिव लेंस (progressive lenses) भी उपलब्ध हैं।
- अबिंदुकता (Astigmatism): यह दोष कॉर्निया या नेत्र लेंस के अनियमित आकार के कारण होता है, जिसके कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएँ एक साथ फोकस नहीं हो पाती हैं। इसके कारण धुंधली दृष्टि होती है।
- संशोधन: इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस (cylindrical lenses) का उपयोग किया जाता है।
- निकट दृष्टि दोष (Myopia) या लघुदृष्टि: इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि:
- कुछ कारणों से नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है, जिसके कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ सामान्य दृष्टि दोष निम्नलिखित हैं:
- प्रकाश का अपवर्तन – कांच के प्रिज्म से अपवर्तन (Refraction of Light through a Glass Prism):
- प्रिज्म दो त्रिकोणीय आधारों और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है।
- जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, तो यह दो बार अपवर्तित होती है – एक बार जब यह प्रिज्म में प्रवेश करती है और दूसरी बार जब यह प्रिज्म से बाहर निकलती है।
- आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण (emergent ray) एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण (Angle of Deviation, δ) कहते हैं। यह आपतन कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है।
- प्रकाश का वर्ण विक्षेपण (Dispersion of White Light):
- जब श्वेत प्रकाश (जैसे सूर्य का प्रकाश) किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो यह अपने घटक रंगों (सात रंग – VIBGYOR: Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red) में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग-अलग होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है।
- स्पेक्ट्रम (Spectrum): रंगों का यह बैंड जो श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है।
- वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction):
- पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान अलग-अलग होता है, जिसके कारण उनका अपवर्तनांक भी अलग-अलग होता है। जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो यह लगातार अपवर्तित होता रहता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं।
- वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ प्रभाव:
- तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars): तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, तो वायुमंडल की परतों के बदलते घनत्व के कारण लगातार अपवर्तित होता रहता है। इससे तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और उनकी चमक बदलती हुई दिखाई देती है, जिसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ग्रह पृथ्वी के बहुत पास हैं और वे प्रकाश के बड़े स्रोत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव उन पर औसतन शून्य होता है और वे टिमटिमाते नहीं हैं।
- अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त (Advance Sunrise and Delayed Sunset): सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, तो उससे आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है।
- आभासी चपटा आकार (Apparent Flattening of the Sun at Sunrise and Sunset): क्षितिज के पास वायुमंडल की परतों का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश का अधिक अपवर्तन होता है। इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है।
- प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light):
- जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें बहुत छोटे-छोटे कण (जैसे वायु के अणु, धूल के कण) होते हैं, तो ये कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
- प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत छोटे कण मुख्य रूप से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश (जैसे नीला) को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े कण अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को भी प्रकीर्णित कर सकते हैं।
- प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण:
- आकाश का नीला रंग (Blue Colour of the Sky): सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए वायुमंडल के छोटे कण इसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है।
- सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग (Red Colour of the Sun at Sunrise and Sunset): सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है और प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस दौरान नीले रंग का प्रकाश अधिकांशतः प्रकीर्णित हो जाता है और केवल अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आँखों तक पहुँच पाता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है।
- खतरे के सिग्नल का लाल रंग (Red Colour of Danger Signals): लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं।
- अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है (Sky Appears Dark to Astronauts): अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश काला दिखाई देता है।
सारांश:
इस अध्याय में हमने मानव नेत्र की संरचना और कार्य, समंजन क्षमता, दृष्टि दोष और उनके संशोधन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन किया। यह ज्ञान हमें हमारे आसपास के रंगबिरंगे संसार और प्रकाश से जुड़ी विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करता है।
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु:
- नेत्रदान एक महान कार्य है जो किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दुनिया देखने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए और किसी भी समस्या होने पर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।