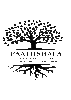अध्याय 3: धातु एवं अधातु
- परिचय
- धातु
- भौतिक गुण
- रासायनिक गुण
- अधातु
- भौतिक गुण
- रासायनिक गुण
- धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर
- धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी
- आयनिक यौगिकों का निर्माण
- आयनिक यौगिकों के गुण
- धातुओं की प्राप्ति
- अयस्कों का समृद्धिकरण
- धातुओं का निष्कर्षण
- कम अभिक्रियाशील धातुएँ
- मध्यम अभिक्रियाशील धातुएँ
- अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ
- धातुओं का परिष्करण
- संक्षारण
- उदाहरण
- संक्षारण से बचाव के तरीके
- सारांश
- अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु
धातु एवं अधातु
परिचय:
यह अध्याय हमें हमारे आसपास मौजूद पदार्थों को दो मुख्य श्रेणियों – धातु और अधातु – में वर्गीकृत करने और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को समझने में मदद करता है। यह नोट्स NCERT की पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री पर आधारित हैं ताकि आपको विषय को आसानी से समझने में मदद मिल सके।
मुख्य विषय:
- धातु (Metals):
- भौतिक गुण (Physical Properties):
- चमक (Lustre): धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं।
- कठोरता (Hardness): अधिकांश धातुएँ कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटैशियम जैसी धातुएँ नरम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है।
- आघातवर्धनीयता (Malleability): धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है।
- तन्यता (Ductility): धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं।
- ऊष्मा और विद्युत के सुचालक (Conductors of Heat and Electricity): धातुएँ ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं। चांदी सबसे अच्छी चालक है, उसके बाद तांबा और एल्युमीनियम।
- ध्वनि (Sonorous): धातुओं को टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है।
- अवस्था (State): कमरे के तापमान पर अधिकांश धातुएँ ठोस होती हैं, लेकिन पारा (Mercury) द्रव अवस्था में होता है।
- उच्च गलनांक और क्वथनांक (High Melting and Boiling Points): अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटैशियम के अपेक्षाकृत कम होते हैं।
- रासायनिक गुण (Chemical Properties):
- ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया: धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
- उदाहरण: 2Mg(s)+O2(g)→2MgO(s) (मैग्नीशियम ऑक्साइड – क्षारीय)
- कुछ धातुएँ अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग ऑक्साइड बनाती हैं (जैसे आयरन FeO, Fe2O3, Fe3O4 बनाता है)।
- उभयधर्मी ऑक्साइड (Amphoteric Oxides): कुछ धातु ऑक्साइड (जैसे एल्युमीनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO) अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण दिखाते हैं। ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं।
- Al2O3(s)+6HCl(aq)→2AlCl3(aq)+3H2O(l) (अम्ल के साथ अभिक्रिया)
- Al2O3(s)+2NaOH(aq)→Na2AlO2(aq)+H2O(l) (सोडियम एल्युमिनेट – क्षारक के साथ अभिक्रिया)
- जल के साथ अभिक्रिया: धातुएँ जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अभिक्रिया की दर धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है।
- सोडियम और पोटैशियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएँ ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं।
- 2Na(s)+2H2O(l)→2NaOH(aq)+H2(g)+ऊष्मा
- मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है या भाप के साथ तेजी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है।
- Mg(s)+H2O(g)→MgO(s)+H2(g)
- एल्युमीनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएँ न तो ठंडे और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं।
- 3Fe(s)+4H2O(g)→Fe3O4(s)+4H2(g)
- लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएँ जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं।
- सोडियम और पोटैशियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएँ ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं।
- अम्लों के साथ अभिक्रिया: धातुएँ तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं।
- Mg(s)+2HCl(aq)→MgCl2(aq)+H2(g)
- नाइट्रिक अम्ल (HNO3) के साथ अभिक्रिया करने पर आमतौर पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और H2 को जल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड (N2O, NO, NO2) में अपचयित हो जाता है।
- अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया: अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवणों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं (विस्थापन अभिक्रिया)। यह धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित है।
- ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया: धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
- भौतिक गुण (Physical Properties):
- अधातु (Non-Metals):
- भौतिक गुण (Physical Properties):
- चमकहीन (Non-Lustrous): इनमें धात्विक चमक नहीं होती है (आयोडीन और ग्रेफाइट अपवाद हैं)।
- नरम (Soft): अधिकांश अधातुएँ नरम होती हैं (हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है)।
- भंगुर (Brittle): पीटने या खींचने पर आसानी से टूट जाती हैं।
- ऊष्मा और विद्युत के कुचालक (Poor Conductors of Heat and Electricity): ये ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती हैं (ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है)।
- अध्वनिक (Non-Sonorous): टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं।
- अवस्था (State): कमरे के तापमान पर ठोस (जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस), द्रव (जैसे ब्रोमीन) या गैस (जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन) अवस्था में हो सकती हैं।
- निम्न गलनांक और क्वथनांक (Low Melting and Boiling Points): अधिकांश अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं (हीरा और ग्रेफाइट के उच्च होते हैं)।
- रासायनिक गुण (Chemical Properties):
- ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया: अधातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या उदासीन होते हैं।
- उदाहरण: C(s)+O2(g)→CO2(g) (कार्बन डाइऑक्साइड – अम्लीय)
- S(s)+O2(g)→SO2(g) (सल्फर डाइऑक्साइड – अम्लीय)
- 2H2(g)+O2(g)→2H2O(l) (जल – उदासीन)
- जल के साथ अभिक्रिया: सामान्यतः अधातुएँ जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं।
- अम्लों के साथ अभिक्रिया: सामान्यतः अधातुएँ तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं।
- क्षारकों के साथ अभिक्रिया: कुछ अधातुएँ क्षारकों के साथ जटिल अभिक्रिया करती हैं।
- उदाहरण: 2NaOH(aq)+Si(s)+H2O(l)→Na2SiO3(aq)+2H2(g) (सोडियम सिलिकेट)
- ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया: अधातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या उदासीन होते हैं।
- भौतिक गुण (Physical Properties):
- धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर (Difference Between Metals and Non-Metals):
| गुण | धातु | अधातु | | ——————– | —————————————- | ——————————————- | | चमक | चमकदार | चमकहीन (आयोडीन, ग्रेफाइट अपवाद) | | कठोरता | सामान्यतः कठोर (Na, K अपवाद) | सामान्यतः नरम (हीरा अपवाद) | | आघातवर्धनीयता | आघातवर्धनीय | भंगुर | | तन्यता | तन्य | अतन्य | | चालकता (ऊष्मा/विद्युत) | अच्छे चालक | कुचालक (ग्रेफाइट अपवाद) | | ध्वनिकता | ध्वनिक | अध्वनिक | | अवस्था (कमरे के ताप पर) | ठोस (पारा अपवाद) | ठोस, द्रव या गैस | | ऑक्साइड की प्रकृति | क्षारीय या उभयधर्मी | अम्लीय या उदासीन | | आयन बनाने की प्रवृत्ति | धनायन बनाते हैं (इलेक्ट्रॉन त्यागकर) | ऋणायन बनाते हैं (इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके) |
- धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity Series of Metals):
- यह धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने वाली सूची है।
- इस श्रेणी का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कौन सी धातु दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है।
- अभिक्रियाशीलता क्रम: पोटैशियम (K) > सोडियम (Na) > कैल्शियम (Ca) > मैग्नीशियम (Mg) > एल्युमीनियम (Al) > जिंक (Zn) > आयरन (Fe) > लेड (Pb) > हाइड्रोजन (H) > कॉपर (Cu) > मर्करी (Hg) > सिल्वर (Ag) > गोल्ड (Au)
- याद रखने की तरकीब (उदाहरण): Kedar Nath Ca Mali Aaloo Zara Feeke Pakata Hai, Con Hai Aapka.
- आयनिक यौगिकों का निर्माण (Formation of Ionic Compounds):
- धातुएँ इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन (धनात्मक आयन) बनाती हैं और अधातुएँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन (ऋणात्मक आयन) बनाती हैं।
- विपरीत आवेश वाले आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़कर आयनिक यौगिक बनाते हैं।
- उदाहरण: सोडियम क्लोराइड (NaCl) का निर्माण:
- सोडियम (Na) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास: 2, 8, 1 (एक इलेक्ट्रॉन त्यागकर Na+ बनाता है)
- क्लोरीन (Cl) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास: 2, 8, 7 (एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl− बनाता है)
- Na++Cl−→NaCl
- आयनिक यौगिकों के गुण (Properties of Ionic Compounds):
- भौतिक अवस्था: ठोस
- गलनांक और क्वथनांक: उच्च
- विलेयता: सामान्यतः जल में घुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील
- विद्युत चालकता: ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं (मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण)।
- धातुओं की प्राप्ति (Extraction of Metals):
- पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुएँ यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें अयस्क (Ores) कहते हैं।
- अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म (Metallurgy) कहलाती है। इसमें कई चरण शामिल होते हैं जो धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं।
- अयस्कों का समृद्धिकरण (Enrichment of Ores): अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों (गैंग – Gangue) को दूर करना। इसके लिए विभिन्न विधियाँ उपयोग की जाती हैं, जैसे गुरुत्व पृथक्करण, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, रासायनिक निक्षालन।
- धातुओं का निष्कर्षण (Extraction of Metals):
- कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण: ये धातुएँ प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं (जैसे सोना, चांदी)। इनके अयस्कों को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त की जा सकती है (जैसे मर्करी सल्फाइड से मर्करी)।
- HgS(s)+O2(g)→HgO(s)+SO2(g)
- 2HgO(s)Δ2Hg(l)+O2(g)
- मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण: ये धातुएँ ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। निष्कर्षण से पहले इन्हें ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
- भर्जन (Roasting): सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना।
- 2ZnS(s)+3O2(g)Δ2ZnO(s)+2SO2(g)
- निस्तापन (Calcination): कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना।
- ZnCO3(s)ΔZnO(s)+CO2(g)
- फिर धातु ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक (जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड) का उपयोग करके धातु में अपचयित किया जाता है।
- ZnO(s)+C(s)→Zn(s)+CO(g)
- भर्जन (Roasting): सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना।
- अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण: इन धातुओं (जैसे सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमीनियम) को उनके गलित क्लोराइड या ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्योंकि ये कार्बन जैसे सामान्य अपचायकों द्वारा अपचयित नहीं किए जा सकते हैं।
- उदाहरण: गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन: 2NaCl(l)विद्युत अपघटन2Na(s)+Cl2(g)
- उदाहरण: गलित एल्युमिना (Al2O3) का विद्युत अपघटन (क्रायोलाइट मिलाकर गलनांक कम किया जाता है)।
- कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण: ये धातुएँ प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं (जैसे सोना, चांदी)। इनके अयस्कों को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त की जा सकती है (जैसे मर्करी सल्फाइड से मर्करी)।
- धातुओं का परिष्करण (Refining of Metals): प्राप्त धातु में अभी भी कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए परिष्करण की आवश्यकता होती है। विद्युत अपघटनी परिष्करण एक सामान्य विधि है जिसका उपयोग कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुओं के लिए किया जाता है।
- संक्षारण (Corrosion):
- धातुओं का वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है।
- उदाहरण:
- लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron): लोहा (Fe) वायु में ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड (Fe2O3.xH2O) बनाता है, जो जंग कहलाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक हैं।
- चांदी पर काली परत चढ़ना (Ag2S)
- तांबे पर हरी परत चढ़ना (CuCO3.Cu(OH)2)
- संक्षारण से बचाव के तरीके (Prevention of Corrosion):
- पेंट करना
- तेल लगाना
- ग्रीस लगाना
- गैल्वनीकरण (Galvanization): लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाना। जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण पहले संक्षारित होता है और लोहे को बचाता है।
- विद्युत लेपन (Electroplating)
- मिश्र धातु बनाना (Alloying): दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने से धातु के गुणों में सुधार किया जा सकता है (जैसे कठोरता, संक्षारण प्रतिरोध)।
- उदाहरण: स्टेनलेस स्टील (लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन) जंगरोधी होता है।
- पीतल (तांबा और जस्ता)
- कांसा (तांबा और टिन)
सारांश:
इस अध्याय में हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों, उनके बीच के अंतर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, आयनिक यौगिकों के निर्माण और गुणों, धातुओं की प्राप्ति की विभिन्न प्रक्रियाओं (अयस्क का समृद्धिकरण, निष्कर्षण और परिष्करण) और संक्षारण तथा उससे बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। यह ज्ञान हमें हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और विभिन्न पदार्थों के उपयोगों को जानने में मदद करता है।
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु:
- मिश्र धातुओं का उपयोग उनके बेहतर गुणों के कारण व्यापक रूप से किया जाता है।
- धातुओं का निष्कर्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है।
- संक्षारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे धातुओं को नुकसान होता है और इससे बचाव के उपाय महत्वपूर्ण हैं।