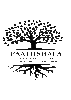अध्याय 5: जीवन की मौलिक इकाई –
विषय सूची:
- कोशिका क्या है?
- जीवन की आधारभूत इकाई
- कोशिका की खोज
- कोशिका सिद्धांत
- कोशिकाओं का आकार और आकृति
- एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव
- कोशिका की संरचना
- कोशिका झिल्ली (Plasma Membrane)
- कार्य
- चयनात्मक पारगम्यता
- विसरण और परासरण
- कोशिका भित्ति (Cell Wall)
- कार्य
- पादप कोशिकाओं में
- केंद्रक (Nucleus)
- संरचना
- कार्य
- क्रोमोसोम और डीएनए
- कोशिका द्रव्य (Cytoplasm)
- संरचना
- कार्य
- कोशिका अंगक (Cell Organelles)
- अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum – ER)
- खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका (Rough ER)
- चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका (Smooth ER)
- कार्य
- गॉल्जी उपकरण (Golgi Apparatus)
- संरचना
- कार्य
- लाइसोसोम (Lysosomes)
- संरचना
- कार्य
- माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)
- संरचना
- कार्य
- प्लास्टिड (Plastids)
- क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast)
- क्रोमोप्लास्ट (Chromoplast)
- ल्यूकोप्लास्ट (Leucoplast)
- कार्य
- रिक्तिकाएँ (Vacuoles)
- संरचना
- कार्य
- अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum – ER)
- कोशिका झिल्ली (Plasma Membrane)
- कोशिका विभाजन (Cell Division)
- समसूत्री विभाजन (Mitosis)
- अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis)
- महत्व
विस्तृत नोट्स:
- कोशिका क्या है?
- जीवन की आधारभूत इकाई: कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक आधारभूत इकाई है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं या एक अकेली कोशिका से बने होते हैं। जिस प्रकार ईंटें मिलकर एक इमारत बनाती हैं, उसी प्रकार कोशिकाएँ मिलकर एक जीव का शरीर बनाती हैं और उसके सभी कार्यों को संपन्न करती हैं।
- कोशिका की खोज:
- रॉबर्ट हुक (Robert Hooke, 1665): इन्होंने स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएँ देखीं और इन्हें ‘कोशिका’ (Cell) नाम दिया। यहाँ ‘सेल’ का अर्थ एक छोटा कमरा था।
- एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक (Anton van Leeuwenhoek, 1674): इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं (जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ) को देखा।
- कोशिका सिद्धांत (Cell Theory):
- श्लीडेन (Schleiden, 1838) और श्वान (Schwann, 1839): इन दो जीववैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं।
- विरचो (Virchow, 1855): इन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि नई कोशिकाएँ पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं (“Omnis cellula e cellula”)।
- आधुनिक कोशिका सिद्धांत:
- सभी जीवित जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं।
- कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
- सभी कोशिकाएँ पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं।
- कोशिकाओं का आकार और आकृति: कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग होती है। कुछ कोशिकाएँ गोलाकार, कुछ लंबी, कुछ शाखाओं वाली और कुछ अनियमित आकार की होती हैं। इनका आकार कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है (जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा)।
- एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव:
- एककोशिकीय जीव (Unicellular Organisms): वे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। यह अकेली कोशिका ही उनके सभी जीवन कार्यों को संपन्न करती है। उदाहरण: अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट।
- बहुकोशिकीय जीव (Multicellular Organisms): वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन जीवों में अलग-अलग कार्य करने के लिए कोशिकाओं के समूह (ऊतक, अंग, अंग तंत्र) पाए जाते हैं। उदाहरण: पौधे, जंतु, कवक।
- कोशिका की संरचना:
एक प्रारूपिक कोशिका में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं:
- कोशिका झिल्ली (Plasma Membrane):
- यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है (जंतु कोशिकाओं में) या कोशिका भित्ति के अंदर होती है (पादप कोशिकाओं में)।
- यह एक पतली, लचीली और जीवित झिल्ली होती है जो लिपिड (वसा) और प्रोटीन से बनी होती है।
- कार्य:
- कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है।
- कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है।
- कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है।
- चयनात्मक पारगम्यता (Selectively Permeable): कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है, जबकि कुछ को नहीं। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।
- विसरण (Diffusion): पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करना विसरण कहलाता है। गैसों (जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड) का कोशिका झिल्ली के आर-पार आवागमन विसरण द्वारा होता है।
- परासरण (Osmosis): जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली (जैसे कोशिका झिल्ली) से अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना परासरण कहलाता है। यह विसरण का ही एक विशेष प्रकार है जिसमें केवल जल के अणु गति करते हैं। परासरण तीन प्रकार के विलयनों पर निर्भर करता है:
- अल्पपरासारी विलयन (Hypotonic Solution): यदि कोशिका के बाहर का विलयन कोशिका के अंदर के विलयन की तुलना में कम सांद्रित (कम घुला हुआ पदार्थ) हो, तो जल कोशिका में प्रवेश करेगा और कोशिका फूल जाएगी (स्फीति)।
- समपरासारी विलयन (Isotonic Solution): यदि कोशिका के बाहर और अंदर के विलयन की सांद्रता समान हो, तो जल का कोशिका में आना-जाना संतुलित रहेगा और कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- अतिपरासारी विलयन (Hypertonic Solution): यदि कोशिका के बाहर का विलयन कोशिका के अंदर के विलयन की तुलना में अधिक सांद्रित (अधिक घुला हुआ पदार्थ) हो, तो कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी (जीवद्रव्यकुंचन)।
- कोशिका भित्ति (Cell Wall):
- यह पादप कोशिकाओं, कवक और बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली एक कठोर और निर्जीव परत होती है।
- पादप कोशिकाओं में यह मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है।
- कार्य:
- कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता और आकार प्रदान करती है।
- कोशिका को बाहरी आघातों और परिवर्तनों से बचाती है।
- कोशिका को फूलने से (अतिपरासारी विलयन में) रोकती है।
- केंद्रक (Nucleus):
- यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है, जिसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है।
- यह आमतौर पर कोशिका के मध्य में स्थित होता है (कुछ कोशिकाओं में किनारे पर भी हो सकता है)।
- संरचना:
- केंद्रक झिल्ली (Nuclear Membrane): यह दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जिसमें छोटे-छोटे छिद्र (केंद्रक छिद्र) होते हैं जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं।
- केंद्रक द्रव्य (Nucleoplasm): यह केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है।
- केंद्रिका (Nucleolus): यह केंद्रक के अंदर एक छोटी, गोलाकार संरचना होती है जो राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है।
- क्रोमैटिन (Chromatin): यह धागे जैसी संरचनाओं का जाल होता है जो डीएनए (Deoxyribonucleic Acid) और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन संघनित होकर क्रोमोसोम (Chromosomes) बनाते हैं।
- कार्य:
- कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- आनुवंशिक सूचना (डीएनए) को धारण करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है।
- कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राइबोसोम का निर्माण करता है।
- क्रोमोसोम और डीएनए: क्रोमोसोम में डीएनए अणु होते हैं। डीएनए में आनुवंशिक जानकारी निहित होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। डीएनए खंड जो किसी कार्य विशेष के लिए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना रखते हैं, जीन (Genes) कहलाते हैं।
- कोशिका द्रव्य (Cytoplasm):
- यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा तरल पदार्थ है।
- संरचना: इसमें पानी, लवण, कार्बनिक अणु (जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा) और विभिन्न कोशिका अंगक (राइबोसोम को छोड़कर) निलंबित रहते हैं।
- कार्य:
- कोशिका अंगकों के लिए माध्यम प्रदान करता है।
- कई चयापचय (metabolic) अभिक्रियाएँ कोशिका द्रव्य में ही होती हैं।
- कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है।
- कोशिका अंगक (Cell Organelles): कोशिका द्रव्य में विभिन्न छोटी-छोटी संरचनाएँ पाई जाती हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक का अपना विशिष्ट कार्य होता है।
- अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum – ER):
- यह झिल्लीदार नलिकाओं और शीटों का एक बड़ा नेटवर्क है जो कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैला रहता है।
- दो प्रकार की होती है:
- खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका (Rough ER – RER): इसकी सतह पर राइबोसोम नामक छोटे कण जुड़े होते हैं, जिसके कारण यह खुरदरी दिखाई देती है।
- चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका (Smooth ER – SER): इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है।
- कार्य:
- RER: प्रोटीन संश्लेषण और उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में भेजने में मदद करती है। यह प्रोटीन के फोल्डिंग और रूपांतरण में भी भूमिका निभाती है।
- SER: वसा (लिपिड) और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में मदद करती है। यह विषैले पदार्थों को निराविष (detoxify) करने में भी मदद करती है।
- गॉल्जी उपकरण (Golgi Apparatus):
- यह झिल्लीदार थैलियों (सिस्टर्नी) की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं।
- संरचना: इसके तीन मुख्य भाग होते हैं: सिस्टर्नी, पुटिकाएँ (vesicles)।
- कार्य:
- यह ER में संश्लेषित प्रोटीनों और वसाओं को संसाधित (process), पैक और कोशिका के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करता है।
- यह लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल होता है।
- पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है।
- लाइसोसोम (Lysosomes):
- यह झिल्ली से घिरी हुई छोटी थैलियाँ होती हैं जिनमें पाचक एंजाइम (digestive enzymes) भरे होते हैं। इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली (suicidal bags) भी कहा जाता है।
- संरचना: झिल्ली से घिरी हुई थैली जिसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं।
- कार्य:
- कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस) और खराब हो चुके कोशिका अंगकों को पचाकर साफ करते हैं।
- कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने एंजाइमों द्वारा पूरी कोशिका को पचा लेते हैं।
- माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria):
- यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है जबकि भीतरी झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर उंगली जैसी संरचनाएँ बनाती है जिन्हें क्रिस्टी (cristae) कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह (powerhouse) कहा जाता है।
- संरचना: दोहरी झिल्ली (बाहरी और भीतरी), क्रिस्टी, मैट्रिक्स (भीतरी झिल्ली से घिरा तरल पदार्थ)।
- कार्य: कोशिकीय श्वसन (cellular respiration) द्वारा ऊर्जा (एटीपी – Adenosine Triphosphate के रूप में) उत्पन्न करना। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है, इसलिए यह कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है।
- प्लास्टिड (Plastids):
- यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्लीदार अंगक हैं। इनके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है।
- तीन मुख्य प्रकार के होते हैं:
- क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast): इनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल (chlorophyll) होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह पत्तियों और हरे तनों में पाया जाता है।
- कार्य: प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन (ग्लूकोज) का निर्माण करना।
- क्रोमोप्लास्ट (Chromoplast): इनमें विभिन्न रंगीन वर्णक (जैसे कैरोटीन, जैंथोफिल) होते हैं जो फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं।
- कार्य: फूलों और फलों को रंग प्रदान करना, परागण और बीज प्रकीर्णन में मदद करना।
- ल्यूकोप्लास्ट (Leucoplast): यह रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो भोजन (जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन) का भंडारण करते हैं। यह जड़ों और भूमिगत तनों में पाए जाते हैं।
- कार्य: भोजन का भंडारण करना।
- क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast): इनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल (chlorophyll) होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह पत्तियों और हरे तनों में पाया जाता है।
- रिक्तिकाएँ (Vacuoles):
- यह झिल्ली से घिरी हुई बड़ी या छोटी थैलियाँ होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में आमतौर पर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है।
- संरचना: झिल्ली से घिरी हुई थैली जिसमें जल, खनिज लवण, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ आदि भरे होते हैं। पादप कोशिका की रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली को टोनोप्लास्ट (tonoplast) कहते हैं।
- कार्य:
- कोशिका को स्फीत (turgid) बनाए रखने में मदद करती है।
- अपशिष्ट पदार्थों और जल को संग्रहित करती है।
- पादप कोशिकाओं में अमीनो अम्ल, शर्करा, लवण और प्रोटीन जैसे पदार्थों का भंडारण करती है।
- एककोशिकीय जीवों में भोजन रिक्तिकाएँ भोजन को पचाने में मदद करती हैं।
- अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum – ER):
- कोशिका विभाजन (Cell Division):
नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन दो मुख्य प्रकार का होता है:
- समसूत्री विभाजन (Mitosis): इस प्रकार के विभाजन में एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाएँ बनाती है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका के समान होती है।
- महत्व:
- बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है।
- क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन में मदद करता है।
- एककोशिकीय जीवों में प्रजनन का एक तरीका है।
- महत्व:
- अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis): इस प्रकार के विभाजन में एक जनक कोशिका विभाजित होकर चार पुत्री कोशिकाएँ बनाती है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। यह केवल लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं (जैसे शुक्राणु और अंडाणु) में होता है।
- महत्व:
- युग्मकों (gametes) का निर्माण करता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है।
- लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों में आनुवंशिक विविधता लाता है।
- महत्व: