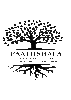अध्याय 5: जैव प्रक्रम
- परिचय
- जैव प्रक्रम क्या हैं?
- पोषण
- स्वपोषी पोषण
- प्रकाश संश्लेषण
- रसायन संश्लेषण
- विषमपोषी पोषण
- मृतजीवी पोषण
- परजीवी पोषण
- प्राणीसम पोषण
- स्वपोषी पोषण
- मनुष्य में पोषण
- पाचन तंत्र
- विभिन्न अंगों में पाचन
- श्वसन
- वायवीय श्वसन
- अवायवीय श्वसन
- पौधों में श्वसन
- जंतुओं में श्वसन
- मनुष्य में श्वसन
- श्वसन तंत्र
- श्वसन की प्रक्रिया
- परिवहन
- पौधों में परिवहन
- जंतुओं में परिवहन
- मनुष्य में परिसंचरण तंत्र
- हृदय
- रक्त वाहिकाएँ
- रक्त
- लसीका तंत्र
- उत्सर्जन
- पौधों में उत्सर्जन
- जंतुओं में उत्सर्जन
- मनुष्य में उत्सर्जन
- उत्सर्जन तंत्र
- वृक्क की संरचना और कार्य
- मूत्र निर्माण की प्रक्रिया
- कृत्रिम वृक्क (अपोहन)
- सारांश
- अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु
जैव प्रक्रम – विस्तृत नोट्स (CBSE, NCERT आधारित)
परिचय:
यह अध्याय हमें उन मूलभूत प्रक्रियाओं के बारे में बताता है जो एक जीवित जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। इन प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम (Life Processes) कहा जाता है। यह नोट्स NCERT की पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री पर आधारित हैं ताकि आपको विषय को आसानी से समझने में मदद मिल सके।
मुख्य विषय:
- जैव प्रक्रम क्या हैं? (What are Life Processes?):
- वे सभी मूलभूत कार्य जो जीवों को जीवित रहने और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए करने पड़ते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
- इनमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- पोषण (Nutrition):
- परिभाषा: भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने और शरीर के रखरखाव के लिए करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है।
- पोषण के प्रकार (Types of Nutrition):
- स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition): वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं (अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं)।
- प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis): हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन (ग्लूकोज) बनाते हैं।
- समीकरण: 6CO2+6H2Oसूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिलC6H12O6+6O2
- प्रक्रिया: यह क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है, जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होता है:
- प्रकाश अभिक्रिया (Light Reaction): यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना (Grana) में होती है। प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है और जल का अपघटन होकर ऑक्सीजन, ATP (एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट) और NADPH (निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट) बनते हैं।
- अंधकार अभिक्रिया (Dark Reaction) या केल्विन चक्र (Calvin Cycle): यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा (Stroma) में होती है। ATP और NADPH का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है।
- रसायन संश्लेषण (Chemosynthesis): कुछ बैक्टीरिया रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं (उदाहरण: सल्फर बैक्टीरिया)।
- प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis): हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन (ग्लूकोज) बनाते हैं।
- विषमपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition): वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं।
- मृतजीवी पोषण (Saprotrophic Nutrition): वे जीव जो मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं (उदाहरण: कवक, कुछ बैक्टीरिया)।
- परजीवी पोषण (Parasitic Nutrition): वे जीव जो अन्य जीवित जीवों (परपोषी – Host) से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं (उदाहरण: जूँ, अमरबेल, फीताकृमि)।
- प्राणीसम पोषण (Holozoic Nutrition): वे जीव जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उसे पचाते हैं (उदाहरण: अमीबा, मनुष्य)। इसमें पाँच चरण शामिल हैं:
- अंतर्ग्रहण (Ingestion): भोजन को शरीर के अंदर लेना।
- पाचन (Digestion): जटिल भोजन अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ना।
- अवशोषण (Absorption): पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषित होना।
- स्वांगीकरण (Assimilation): अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि और मरम्मत के लिए करना।
- बहिष्करण (Egestion): अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना।
- स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition): वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं (अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं)।
- मनुष्य में पोषण (Nutrition in Human Beings):
- मनुष्य में प्राणीसम पोषण होता है।
- पाचन तंत्र (Digestive System): यह एक लंबी नली है जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है और इसमें विभिन्न अंग और ग्रंथियाँ शामिल हैं जो पाचन में मदद करती हैं।
- मुख (Mouth): भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दाँत भोजन को चबाते हैं (यांत्रिक पाचन)। लार ग्रंथियाँ लार (Saliva) स्त्रावित करती हैं जिसमें एमाइलेज (Amylase) एंजाइम होता है जो स्टार्च का आंशिक पाचन करता है (रासायनिक पाचन)।
- ग्रसिका (Oesophagus): यह भोजन नली है जो भोजन को मुख से आमाशय तक क्रमाकुंचन (Peristalsis) गति द्वारा पहुँचाती है।
- आमाशय (Stomach): यह एक जे-आकार का अंग है जहाँ भोजन लगभग 3 घंटे तक मथा जाता है। यहाँ जठर ग्रंथियाँ (Gastric glands) जठर रस स्त्रावित करती हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), पेप्सिन (Pepsin) एंजाइम (प्रोटीन का पाचन) और श्लेष्मा (Mucus) होता है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है, जबकि श्लेष्मा आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है।
- छोटी आंत (Small Intestine): यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। यह तीन भागों में विभाजित है:
- ग्रहणी (Duodenum): यहाँ यकृत (Liver) से पित्त रस (Bile juice) और अग्न्याशय (Pancreas) से अग्न्याशयिक रस (Pancreatic juice) आता है। पित्त रस वसा का इमल्सीकरण (Emulsification) करता है और अग्न्याशयिक रस में एमाइलेज (कार्बोहाइड्रेट का पाचन), ट्रिप्सिन (प्रोटीन का पाचन) और लाइपेज (वसा का पाचन) एंजाइम होते हैं।
- जेजुनम (Jejunum) और इलियम (Ileum): यहाँ आंत की दीवार में आंत्र रस (Intestinal juice) स्त्रावित होता है जिसमें विभिन्न एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन को पूरा करते हैं। इलियम में विल्ली (Villi) नामक उंगली जैसी संरचनाएँ होती हैं जो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं।
- बड़ी आंत (Large Intestine): यह छोटी आंत से छोटा लेकिन चौड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। अपचित भोजन मलाशय (Rectum) में अस्थायी रूप से जमा होता है और फिर गुदा (Anus) द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है (बहिष्करण)।
- श्वसन (Respiration):
- परिभाषा: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
- श्वसन के प्रकार (Types of Respiration):
- वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration): ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा (ATP) उत्पन्न होती है।
- समीकरण: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+ऊर्जा (ATP)
- अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration): ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पाद अलग-अलग जीवों में भिन्न हो सकते हैं:
- यीस्ट में: ग्लूकोज → एथेनॉल + कार्बन डाइऑक्साइड + ऊर्जा
- हमारी मांसपेशियों में (ऑक्सीजन की कमी होने पर): ग्लूकोज → लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा (लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है)
- वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration): ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा (ATP) उत्पन्न होती है।
- पौधों में श्वसन (Respiration in Plants):
- पौधों में गैसों का आदान-प्रदान रंध्रों (Stomata – पत्तियों पर छोटे छिद्र) और वातरंध्रों (Lenticels – तनों और जड़ों पर छिद्र) के माध्यम से होता है।
- पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं।
- पौधों में श्वसन की दर जंतुओं की तुलना में धीमी होती है।
- जंतुओं में श्वसन (Respiration in Animals):
- विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए अलग-अलग अंग होते हैं जो उनके आवास और जटिलता पर निर्भर करते हैं।
- एककोशिकीय जीव (जैसे अमीबा): शरीर की सतह से विसरण (Diffusion) द्वारा गैसों का आदान-प्रदान होता है।
- कीट (जैसे तिलचट्टा): श्वास रंध्रों (Spiracles) और श्वास नलिकाओं (Tracheae) का जाल होता है जिसके माध्यम से गैसें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती हैं।
- जलीय जीव (जैसे मछली): गलफड़े (Gills) जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में छोड़ते हैं।
- स्थलीय कशेरुकी (जैसे मनुष्य): फेफड़े (Lungs) श्वसन अंग हैं।
- विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए अलग-अलग अंग होते हैं जो उनके आवास और जटिलता पर निर्भर करते हैं।
- मनुष्य में श्वसन (Respiration in Human Beings):
- श्वसन तंत्र (Respiratory System): इसमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं:
- नासा द्वार (Nostrils): हवा शरीर में प्रवेश करती है। यहाँ बाल और श्लेष्मा होते हैं जो धूल के कणों को छानते हैं और हवा को नम करते हैं।
- ग्रसनी (Pharynx): यह मुख और नासा गुहा दोनों से जुड़ी होती है।
- स्वरयंत्र (Larynx) या कंठ (Voice Box): इसमें स्वर रज्जु (Vocal cords) होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
- श्वासनली (Trachea) या वायु नली (Windpipe): यह उपास्थि (Cartilage) के छल्लों से बनी होती है जो इसे पिचकने से बचाते हैं।
- श्वसनी (Bronchi): श्वासनली फेफड़ों में प्रवेश करके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है।
- श्वसनिकाएँ (Bronchioles): श्वसनी आगे चलकर छोटी-छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं।
- वायुकोष्ठिकाएँ (Alveoli) या कूपिकाएँ: ये छोटी-छोटी थैली जैसी संरचनाएँ होती हैं जो श्वसनिकाओं के अंत में पाई जाती हैं। यहीं पर गैसों का आदान-प्रदान (ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त और हवा के बीच विसरण) होता है। वायुकोष्ठिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और इनमें रक्त वाहिकाओं का जाल होता है।
- श्वसन की प्रक्रिया (Mechanism of Breathing): इसमें दो मुख्य चरण शामिल हैं:
- अंतःश्वसन (Inhalation) या श्वास लेना: जब हम सांस लेते हैं, तो डायाफ्राम (Diaphragm) नीचे की ओर चपटा होता है और पसलियों की मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं जिससे छाती गुहा (Thoracic cavity) का आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण फेफड़ों के अंदर दाब कम हो जाता है और बाहर की हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है।
- उच्छ्वास (Exhalation) या श्वास छोड़ना: जब हम सांस छोड़ते हैं, तो डायाफ्राम ऊपर की ओर उठता है और पसलियों की मांसपेशियाँ शिथिल होती हैं जिससे छाती गुहा का आयतन कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों के अंदर दाब बढ़ जाता है और फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है।
- श्वसन तंत्र (Respiratory System): इसमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं:
- परिवहन (Transportation):
- परिभाषा: शरीर में पदार्थों (जैसे भोजन, ऑक्सीजन, जल, अपशिष्ट उत्पाद) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है।
- पौधों में परिवहन (Transportation in Plants):
- पौधों में परिवहन के लिए दो मुख्य संवहन ऊतक (Vascular tissues) होते हैं:
- जाइलम (Xylem): यह जड़ों से जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुँचाता है। जल का परिवहन वाष्पोत्सर्जन खिंचाव (Transpiration pull) के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना है, जो एक खिंचाव उत्पन्न करता है और जड़ों से जल को ऊपर खींचता है।
- फ्लोएम (Phloem): यह पत्तियों में बने भोजन (शर्करा) को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। भोजन का परिवहन स्थानांतरण (Translocation) कहलाता है, जो सक्रिय परिवहन द्वारा होता है (ऊर्जा की आवश्यकता होती है)।
- पौधों में परिवहन के लिए दो मुख्य संवहन ऊतक (Vascular tissues) होते हैं:
- जंतुओं में परिवहन (Transportation in Animals):
- जंतुओं में परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र (Circulatory system) होता है।
- मनुष्य में परिसंचरण तंत्र (Circulatory System in Human Beings): यह हृदय (Heart), रक्त वाहिकाओं (Blood vessels – धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ) और रक्त (Blood) से मिलकर बना होता है।
- हृदय (Heart): यह एक पेशीय अंग है जो रक्त को पंप करता है। इसमें चार कक्ष होते हैं: दो अलिंद (Atria – ऊपरी कक्ष जो रक्त प्राप्त करते हैं) और दो निलय (Ventricles – निचले कक्ष जो रक्त पंप करते हैं)।
- रक्त वाहिकाएँ (Blood Vessels):
- धमनियाँ (Arteries): हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं (फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर जो विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है)। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं।
- शिराएँ (Veins): शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक वापस लाती हैं (फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है)। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें रक्त को वापस बहने से रोकने के लिए वाल्व होते हैं।
- केशिकाएँ (Capillaries): ये बहुत पतली रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। यहीं पर रक्त और कोशिकाओं के बीच पदार्थों (ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, अपशिष्ट) का आदान-प्रदान होता है।
- रक्त (Blood): यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो निम्नलिखित घटकों से बना होता है:
- प्लाज्मा (Plasma): रक्त का तरल भाग जिसमें जल, प्रोटीन, लवण आदि होते हैं।
- लाल रक्त कोशिकाएँ (Red Blood Cells – RBCs): इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
- श्वेत रक्त कोशिकाएँ (White Blood Cells – WBCs): ये शरीर को संक्रमण से बचाती हैं।
- प्लेटलेट्स (Platelets): ये रक्त के थक्के बनने में मदद करती हैं।
- लसीका तंत्र (Lymphatic System): यह भी परिवहन में मदद करता है। लसीका (Lymph) एक तरल है जो ऊतक द्रव से बनता है और इसमें सफेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं। यह अतिरिक्त द्रव को ऊतकों से रक्त में वापस ले जाता है और प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है।
- उत्सर्जन (Excretion):
- परिभाषा: शरीर से हानिकारक और अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है।
- पौधों में उत्सर्जन (Excretion in Plants):
- पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं।
- वे विभिन्न तरीकों से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं:
- ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलते हैं।
- अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकलता है।
- कुछ अपशिष्ट उत्पाद पत्तियों, छालों और फलों में जमा हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं।
- कुछ अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रेजिन के रूप में निकलते हैं।
- जंतुओं में उत्सर्जन (Excretion in Animals):
- विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अलग-अलग अंग होते हैं।
- एककोशिकीय जीव (जैसे अमीबा): शरीर की सतह से विसरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं।
- कीट (जैसे तिलचट्टा): मैलपिघी नलिकाएँ (Malpighian tubules) अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से निकालकर आहार नाल में भेजती हैं।
- जलीय जीव (जैसे मछली): अमोनिया उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाता है।
- स्थलीय कशेरुकी (जैसे मनुष्य): वृक्क (Kidneys) मुख्य उत्सर्जन अंग हैं।
- विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अलग-अलग अंग होते हैं।
- मनुष्य में उत्सर्जन (Excretion in Human Beings):
- उत्सर्जन तंत्र (Excretory System): इसमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं:
- वृक्क (Kidneys): दो बीन के आकार के अंग जो पेट के ऊपरी भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये रक्त को छानकर यूरिया (मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद), अतिरिक्त जल और लवणों को मूत्र के रूप में अलग करते हैं।
- मूत्रवाहिनी (Ureters): ये दो नलिकाएँ हैं जो प्रत्येक वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र ले जाती हैं।
- मूत्राशय (Urinary Bladder): यह एक थैली जैसी संरचना है जहाँ मूत्र अस्थायी रूप से जमा होता है।
- मूत्रमार्ग (Urethra): यह वह नली है जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है।
- वृक्क की संरचना और कार्य (Structure and Function of Kidney):
- प्रत्येक वृक्क में लाखों छोटी छानने वाली इकाइयाँ होती हैं जिन्हें वृक्काणु (Nephrons) कहते हैं।
- वृक्काणु के भाग:
- ग्लोमेरुलस (Glomerulus): रक्त केशिकाओं का गुच्छा जहाँ रक्त छाना जाता है।
- बोमन कैप्सूल (Bowman’s Capsule): यह ग्लोमेरुलस को घेरने वाली प्याले जैसी संरचना है जो छने हुए रक्त को एकत्र करती है (ग्लोमेरुलर निस्पंद – Glomerular filtrate)।
- वृक्क नलिका (Renal Tubule): यह एक लंबी कुंडलित नली है जिसके विभिन्न भाग होते हैं (समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडल
- उत्सर्जन तंत्र (Excretory System): इसमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं: