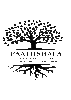अध्याय 2: क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं? –
विषय सूची:
- शुद्ध पदार्थ क्या हैं?
- परिभाषा
- तत्वों और यौगिकों के रूप में शुद्ध पदार्थ
- मिश्रण क्या हैं?
- परिभाषा
- समांगी मिश्रण (Homogeneous Mixtures)
- विषमांगी मिश्रण (Heterogeneous Mixtures)
- विलयन (Solution)
- विलायक और विलेय
- जलीय विलयन
- विलयन के गुणधर्म
- सांद्रता (Concentration)
- द्रव्यमान प्रतिशत
- आयतन प्रतिशत
- संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन
- विलेयता (Solubility)
- निलंबन (Suspension)
- निलंबन के गुणधर्म
- कोलॉइड (Colloid)
- कोलॉइड के गुणधर्म
- टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect)
- कोलॉइड के प्रकार
- परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम
- उदाहरण
- मिश्रणों को पृथक करना
- वाष्पीकरण (Evaporation)
- अपकेन्द्रीकरण (Centrifugation)
- पृथक्करण कीप (Separating Funnel)
- ऊर्ध्वपातन (Sublimation)
- क्रोमैटोग्राफी (Chromatography)
- आसवन (Distillation)
- साधारण आसवन
- प्रभाजी आसवन
- भौतिक और रासायनिक परिवर्तन
- भौतिक परिवर्तन
- रासायनिक परिवर्तन
- भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर
- तत्व (Elements)
- परिभाषा
- धातु (Metals)
- अधातु (Non-metals)
- उपधातु (Metalloids)
- यौगिक (Compounds)
- परिभाषा
- तत्वों और यौगिकों में अंतर
- मिश्रण और यौगिक में अंतर
विस्तृत नोट्स:
- शुद्ध पदार्थ क्या हैं?
- परिभाषा: एक शुद्ध पदार्थ वह होता है जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। इन कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है।
- तत्वों और यौगिकों के रूप में शुद्ध पदार्थ: शुद्ध पदार्थों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
- तत्व (Elements): तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण: लोहा (Fe), सोना (Au), ऑक्सीजन (O), नाइट्रोजन (N)।
- यौगिक (Compounds): यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है। यौगिक के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरण: पानी (H₂O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), नमक (NaCl), चीनी (C₁₂H₂₂O₁₁)।
- मिश्रण क्या हैं?
- परिभाषा: मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों (तत्वों या यौगिकों) को किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिलाने से बनता है। मिश्रण में घटक अपनी पहचान बनाए रखते हैं और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है।
- समांगी मिश्रण (Homogeneous Mixtures): वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और मिश्रण में सभी जगह समान संरचना होती है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसके कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण को विलयन (Solution) भी कहा जाता है। उदाहरण: पानी में चीनी का घोल, हवा, मिश्र धातुएँ (जैसे पीतल – तांबा और जस्ता का मिश्रण)।
- विषमांगी मिश्रण (Heterogeneous Mixtures): वह मिश्रण जिसमें घटक अलग-अलग दिखाई देते हैं और मिश्रण में सभी जगह समान संरचना नहीं होती है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसके कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। उदाहरण: रेत और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, अनाज और कंकड़ का मिश्रण।
- विलयन (Solution):
- विलायक और विलेय: विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है:
- विलायक (Solvent): वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जिसमें दूसरा घटक घुलता है।
- विलेय (Solute): वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और जो विलायक में घुलता है।
- जलीय विलयन: वह विलयन जिसमें विलायक पानी होता है, जलीय विलयन कहलाता है।
- विलयन के गुणधर्म:
- यह एक समांगी मिश्रण है।
- इसके कण बहुत छोटे होते हैं (1 nm से कम व्यास), इसलिए इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है।
- ये प्रकाश के किरणपुंज को नहीं फैलाते हैं क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं।
- विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है।
- ये स्थिर होते हैं, यानी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं।
- सांद्रता (Concentration): विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है:
- द्रव्यमान प्रतिशत (Mass Percentage): विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत=विलयन का द्रव्यमानविलेय का द्रव्यमान×100
- आयतन प्रतिशत (Volume Percentage): विलेय का आयतन प्रतिशत=विलयन का आयतनविलेय का आयतन×100
- संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन:
- संतृप्त विलयन (Saturated Solution): किसी निश्चित तापमान पर, एक विलयन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है।
- असंतृप्त विलयन (Unsaturated Solution): किसी निश्चित तापमान पर, एक विलयन जिसमें विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है।
- अतिसंतृप्त विलयन (Supersaturated Solution): यह एक अस्थिर विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन से भी अधिक विलेय घुला हुआ होता है। इसे विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है।
- विलेयता (Solubility): किसी निश्चित तापमान पर, 100 ग्राम विलायक में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है, उस विलेय की विलायक में विलेयता कहलाती है। तापमान बदलने पर विलेयता बदल जाती है।
- निलंबन (Suspension):
- परिभाषा: निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित (फैले हुए) रहते हैं और नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं।
- निलंबन के गुणधर्म:
- यह एक विषमांगी मिश्रण है।
- इसके कण बड़े होते हैं (100 nm से अधिक व्यास), इसलिए इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है।
- ये प्रकाश के किरणपुंज को फैलाते हैं क्योंकि कण बड़े होते हैं और प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं।
- विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा निलंबन से अलग किया जा सकता है।
- ये अस्थायी होते हैं, यानी कुछ समय बाद विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं।
- कोलॉइड (Colloid):
- परिभाषा: कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन इसके कण विलयन से बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं (1 nm से 100 nm के बीच व्यास)। ये नग्न आँखों से समांगी लगते हैं, लेकिन वास्तव में विषमांगी होते हैं।
- कोलॉइड के गुणधर्म:
- यह विषमांगी होता है।
- इसके कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है।
- ये प्रकाश के किरणपुंज को फैलाते हैं (टिंडल प्रभाव)।
- विलेय के कणों को छानने की सामान्य विधि द्वारा कोलॉइड से अलग नहीं किया जा सकता है।
- ये अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, यानी कण आसानी से नीचे नहीं बैठते हैं।
- टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect): जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइडल विलयन से गुजरती है, तो कोलॉइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण: अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से आने वाली प्रकाश की किरण में धूल के कणों का चमकना, कोहरे में हेडलाइट का चमकना।
- कोलॉइड के प्रकार: कोलॉइड को परिक्षिप्त प्रावस्था (Dispersed Phase) और परिक्षेपण माध्यम (Dispersion Medium) की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:
| परिक्षिप्त प्रावस्था | परिक्षेपण माध्यम | प्रकार | उदाहरण |
| ठोस | ठोस | ठोस सॉल | रंगीन पत्थर, रत्न |
| ठोस | द्रव | सॉल | पेंट, कोशिका द्रव |
| ठोस | गैस | एरोसॉल | धुआँ, धूल |
| द्रव | ठोस | जेल | पनीर, जेली |
| द्रव | द्रव | इमल्शन | दूध, क्रीम, हेयर क्रीम |
| द्रव | गैस | एरोसॉल | कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे |
| गैस | ठोस | ठोस फोम | झांवा पत्थर, रबर स्पंज |
| गैस | द्रव | फोम | साबुन का झाग, शेविंग क्रीम |
- मिश्रणों को पृथक करना:
मिश्रणों के घटकों को उनके भौतिक गुणों में अंतर के आधार पर विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है:
- वाष्पीकरण (Evaporation): इस विधि का उपयोग उन समांगी मिश्रणों से विलेय को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें विलायक वाष्पशील होता है और विलेय अवाष्पशील होता है। उदाहरण: नमक के पानी के घोल से नमक प्राप्त करना।
- अपकेन्द्रीकरण (Centrifugation): इस विधि का उपयोग उन विषमांगी मिश्रणों से ठोस कणों को द्रव से अलग करने के लिए किया जाता है जिनके कण बहुत छोटे होते हैं और आसानी से फिल्टर नहीं किए जा सकते हैं। अपकेन्द्रीकरण में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण: रक्त से रक्त कणिकाओं को अलग करना, दूध से क्रीम निकालना।
- पृथक्करण कीप (Separating Funnel): इस विधि का उपयोग दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके घनत्व अलग-अलग होते हैं। उदाहरण: तेल और पानी के मिश्रण को अलग करना।
- ऊर्ध्वपातन (Sublimation): इस विधि का उपयोग उन मिश्रणों से अवाष्पशील अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है जो ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। उदाहरण: नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना।
- क्रोमैटोग्राफी (Chromatography): इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं और जिनकी विलायक में विलेयता अलग-अलग होती है। उदाहरण: स्याही के रंगों को अलग करना, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना।
- आसवन (Distillation): इस विधि का उपयोग दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होता है। मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे कम क्वथनांक वाला द्रव पहले वाष्पित होता है और फिर संघनित करके अलग कर लिया जाता है।
- साधारण आसवन (Simple Distillation): इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो द्रवों के क्वथनांकों में 25°C से अधिक का अंतर होता है। उदाहरण: पानी और एसीटोन के मिश्रण को अलग करना।
- प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation): इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक द्रवों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। इस विधि में एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है जो वाष्पों को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करता है। उदाहरण: पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों (जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन) को अलग करना, हवा से गैसों को अलग करना।
- भौतिक और रासायनिक परिवर्तन:
- भौतिक परिवर्तन (Physical Change): वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों (जैसे आकार, अवस्था, रंग) में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन अस्थायी हो सकता है और इसे आसानी से उलट भी सकते हैं। उदाहरण: बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का फटना, चीनी का पानी में घुलना।
- रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change): वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनकी रासायनिक संरचना और गुणधर्म मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है और इसे आसानी से उलटा नहीं जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण: लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, दूध से दही बनना।
- भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर:
| गुणधर्म | भौतिक परिवर्तन | रासायनिक परिवर्तन |
| नया पदार्थ बनना | नहीं | हाँ |
| रासायनिक संरचना में परिवर्तन | नहीं | हाँ |
| प्रकृति | अस्थायी हो सकता है | स्थायी |
| ऊर्जा परिवर्तन | आमतौर पर कम | महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन (ऊष्मा, प्रकाश का उत्सर्जन/अवशोषण) |
| उदाहरण | बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, चुंबक बनाना | लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, श्वसन |
- तत्व (Elements):
- परिभाषा: तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
- धातु (Metals): धातुएँ आमतौर पर कठोर, चमकदार, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इन्हें पीटा जा सकता है (आघातवर्धनीयता) और खींचा जा सकता है (तन्यता)। उदाहरण: लोहा, तांबा, सोना, चांदी।
- अधातु (Non-metals): अधातुएँ आमतौर पर नरम, धुंधली, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती हैं। उदाहरण: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर।
- उपधातु (Metalloids): उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। उदाहरण: सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक।
- यौगिक (Compounds):
- परिभाषा: यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है।
- तत्वों और यौगिकों में अंतर:
| गुणधर्म | तत्व | यौगिक |
| संरचना | एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है | दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बना होता है |
| विभाजन | रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता | रासायनिक विधियों द्वारा सरल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है |
| गुणधर्म | अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं | इसके गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं |
| संयोजन | – | तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होता है |
| उदाहरण | लोहा, ऑक्सीजन | पानी (H₂O), नमक (NaCl) |
- मिश्रण और यौगिक में अंतर:
| गुणधर्म | मिश्रण | यौगिक |
| निर्माण | दो या दो से अधिक पदार्थों को भौतिक रूप से मिलाने से बनता है | दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से संयोजन से बनता है |
| घटक | घटक अपनी पहचान बनाए रखते हैं | घटक अपनी पहचान खो देते हैं और नए गुणधर्मों वाला पदार्थ बनाते हैं |
| संयोजन | घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है | तत्वों का एक निश्चित अनुपात में संयोजन होता है |
| पृथक्करण | भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है | रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है |
| गुणधर्म | मिश्रण अपने घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है | यौगिक के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं |
| उदाहरण | रेत और पानी, हवा | पानी, कार्बन डाइऑक्साइड |