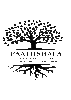अध्याय 12: खाद्य संसाधनों में सुधार Notes
विषय सूची:
- खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता
- बढ़ती जनसंख्या
- सीमित भूमि
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
- गुणवत्ता में सुधार
- फसल उत्पादन का प्रबंधन (Management of Crop Production)
- फसल की किस्में (Crop Varieties)
- उच्च उपज
- बेहतर गुणवत्ता
- जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता
- परिपक्वता अवधि में परिवर्तन
- व्यापक अनुकूलता
- वांछनीय कृषि संबंधी विशेषताएं
- फसल उत्पादन प्रबंधन (Crop Production Management)
- पोषक तत्व प्रबंधन (Nutrient Management)
- आवश्यक पोषक तत्व (मैक्रो और माइक्रो)
- खाद और उर्वरक (Manure and Fertilizers)
- खाद के लाभ
- उर्वरकों के लाभ और हानि
- जैविक खेती (Organic Farming)
- सिंचाई (Irrigation)
- सिंचाई के तरीके
- फसल पैटर्न (Cropping Patterns)
- मिश्रित फसल (Mixed Cropping)
- अंतराफसल (Intercropping)
- फसल चक्र (Crop Rotation)
- फसल सुरक्षा प्रबंधन (Crop Protection Management)
- खरपतवार (Weeds)
- कीट (Pests)
- रोग (Diseases)
- नियंत्रण के तरीके (निवारक और उपचारात्मक)
- जैविक नियंत्रण (Biological Control)
- पोषक तत्व प्रबंधन (Nutrient Management)
- फसल की किस्में (Crop Varieties)
- पशुधन प्रबंधन (Animal Husbandry)
- पशुधन का महत्व
- पशुधन की श्रेणियाँ
- पशुधन प्रबंधन के पहलू
- पशुधन का भोजन (Feeding)
- पशुधन का आश्रय (Shelter)
- पशुधन का प्रजनन (Breeding)
- रोग नियंत्रण (Disease Control)
- कुक्कुट पालन (Poultry Farming)
- अंडे और मांस उत्पादन
- प्रबंधन
- मत्स्य पालन (Fish Farming / Pisciculture)
- मछली के स्रोत
- जलीय कृषि (Aquaculture)
- मत्स्य पालन के प्रकार
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन (Inland Fisheries)
- समुद्री मत्स्य पालन (Marine Fisheries)
- सतत मत्स्य पालन (Sustainable Fisheries)
- मधुमक्खी पालन (Bee-keeping / Apiculture)
- शहद और मोम उत्पादन
- प्रबंधन

विस्तृत नोट्स:
1. खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता:
- बढ़ती जनसंख्या: भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे भोजन की मांग में भी वृद्धि हो रही है।
- सीमित भूमि: खेती योग्य भूमि सीमित है और शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण यह और कम होती जा रही है।
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि: बढ़ती जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है।
- गुणवत्ता में सुधार: केवल मात्रा में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, उत्पादित भोजन की गुणवत्ता (पोषक तत्वों की मात्रा) में भी सुधार करना महत्वपूर्ण है।
- सतत कृषि: हमें ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों और दीर्घकाल तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
2.फसल उत्पादन का प्रबंधन (Management of Crop Production):
फसल उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए तीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है: फसल की किस्में, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये सभी बिंदु खाद्य संसाधनों में सुधार notes का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- फसल की किस्में (Crop Varieties): अच्छी फसल की किस्मों का चयन उत्पादन बढ़ाने का पहला कदम है। वांछित विशेषताओं वाली किस्में विकसित करने के लिए संकरण (hybridization) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अच्छी किस्मों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:
- उच्च उपज: प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में।
- बेहतर गुणवत्ता: उत्पाद में वांछनीय गुणवत्ता वाले पोषक तत्व (जैसे प्रोटीन, तेल, विटामिन) अधिक मात्रा में होने चाहिए।
- जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता: किस्में रोगों, कीटों और अजैविक तनावों (जैसे सूखा, अत्यधिक तापमान, लवणता) के प्रति अधिक प्रतिरोधी होनी चाहिए।
- परिपक्वता अवधि में परिवर्तन: कम समय में पकने वाली किस्में किसानों को एक वर्ष में अधिक फसलें उगाने में मदद करती हैं।
- व्यापक अनुकूलता: किस्में विभिन्न जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों में उगने में सक्षम होनी चाहिए।
- वांछनीय कृषि संबंधी विशेषताएं: बौनापन (cereals में ताकि तेज हवा में न गिरें), अत्यधिक शाखाएँ (चारे वाली फसलों में)।
- फसल उत्पादन प्रबंधन (Crop Production Management): इसमें वे सभी कृषि पद्धतियां शामिल हैं जो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती हैं।
- पोषक तत्व प्रबंधन (Nutrient Management): पौधों को वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
- आवश्यक पोषक तत्व:
- मैक्रो पोषक तत्व (Macro-nutrients): ये पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। उदाहरण: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन (हवा और पानी से मिलते हैं), नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K), कैल्शियम (Ca), मैग्नीशियम (Mg), सल्फर (S)।
- माइक्रो पोषक तत्व (Micro-nutrients): ये पौधों को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। उदाहरण: लोहा (Fe), मैंगनीज (Mn), बोरॉन (B), जिंक (Zn), तांबा (Cu), मोलिब्डेनम (Mo), क्लोरीन (Cl)।
- खाद और उर्वरक (Manure and Fertilizers): मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
- खाद (Manure): यह जैविक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्टों के अपघटन से प्राप्त होता है। यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। खाद के प्रकार:
- कम्पोस्ट (Compost): रसोई के कचरे, खेत के कचरे और पशुधन के गोबर के अपघटन से प्राप्त होता है।
- वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost): केंचुओं का उपयोग करके खाद बनाना।
- हरी खाद (Green Manure): फसल बोने से पहले कुछ फलीदार पौधों को उगाकर मिट्टी में मिला देना।
- उर्वरक (Fertilizers): ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें विशेष पोषक तत्व (जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) उच्च मात्रा में होते हैं। ये पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
- लाभ: उच्च उपज, पौधों की तेजी से वृद्धि।
- हानि: मिट्टी की उर्वरता को दीर्घकाल में कम कर सकते हैं, जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- जैविक खेती (Organic Farming): यह कृषि की वह प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जैविक खाद, जैव उर्वरक और जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके लाभ हैं: मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, स्वस्थ भोजन प्राप्त होता है।
- खाद (Manure): यह जैविक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्टों के अपघटन से प्राप्त होता है। यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। खाद के प्रकार:
- सिंचाई (Irrigation): पौधों को वृद्धि के लिए नियमित रूप से पानी की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। पानी की कमी से फसल की उपज प्रभावित हो सकती है।
- सिंचाई के तरीके (खाद्य संसाधनों में सुधार notes में वर्णित):
- पारंपरिक तरीके: नहरें, तालाब, कुएँ।
- आधुनिक तरीके:
- फव्वारा सिंचाई (Sprinkler Irrigation): पानी को फव्वारे के रूप में पौधों पर छिड़का जाता है।
- ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation): पानी को बूंद-बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह पानी की बचत के लिए बहुत प्रभावी तरीका है।
- फसल पैटर्न (Cropping Patterns): एक ही खेत में अलग-अलग समय पर विभिन्न फसलों को उगाने के तरीके को फसल पैटर्न कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार हैं:
- मिश्रित फसल (Mixed Cropping): एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। उदाहरण: गेहूं और चना, मक्का और दाल। यह जोखिम को कम करता है (एक फसल खराब होने पर दूसरी से आय हो सकती है) और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है।
- अंतराफसल (Intercropping): एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित पंक्तियों या पैटर्न में उगाना। उदाहरण: मक्का और सोयाबीन की पंक्तियाँ। यह पोषक तत्वों के बेहतर उपयोग और कीटों के नियंत्रण में मदद करता है।
- फसल चक्र (Crop Rotation): एक ही खेत में एक निश्चित क्रम में अलग-अलग फसलों को उगाना। उदाहरण: फलीदार फसलों (जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करती हैं) के बाद अनाज की फसलें उगाना। यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और कीटों और रोगों के चक्र को तोड़ता है।
- फसल सुरक्षा प्रबंधन (Crop Protection Management): फसलों को खरपतवारों, कीटों और रोगों से बचाना फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है।
- खरपतवार (Weeds): अवांछित पौधे जो मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश को छीन लेते हैं।
- कीट (Pests): ऐसे जीव जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं (जैसे पत्तियों को खाना, रस चूसना, जड़ों को नुकसान पहुंचाना)।
- रोग (Diseases): सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक) के कारण होने वाली बीमारियाँ जो पौधों की वृद्धि और उपज को प्रभावित करती हैं।
- नियंत्रण के तरीके:
- निवारक उपाय: अच्छी किस्मों का चयन, उचित बीज बोना, फसल चक्र अपनाना, खेत की सफाई रखना।
- उपचारात्मक उपाय:
- यांत्रिक विधियाँ: हाथों से खरपतवार निकालना, कीटों को पकड़ना।
- रासायनिक विधियाँ: खरपतवारनाशकों (weeds को मारने के लिए), कीटनाशकों (pests को मारने के लिए), और कवकनाशकों (fungi को मारने के लिए) का उपयोग करना। इनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- जैविक नियंत्रण (Biological Control): कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं (जैसे परजीवी, शिकारी) का उपयोग करना। उदाहरण: लेडीबर्ड बीटल एफिड्स (aphids) को खाती है। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीका है।
- आवश्यक पोषक तत्व:
- पोषक तत्व प्रबंधन (Nutrient Management): पौधों को वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
3. पशुधन प्रबंधन (Animal Husbandry):
पशुधन प्रबंधन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो पालतू जानवरों (जैसे मवेशी, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, मधुमक्खी) के पालन-पोषण, प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है ताकि उनसे उपयोगी उत्पाद (जैसे दूध, मांस, अंडे, ऊन, शहद) प्राप्त किए जा सकें।
- पशुधन का महत्व: भोजन का स्रोत, आय का स्रोत, कृषि कार्यों में सहायता (जैसे हल चलाना), परिवहन, खाद का स्रोत।
- पशुधन की श्रेणियाँ: मवेशी (गाय, भैंस), भेड़, बकरी, कुक्कुट (मुर्गी, बत्तख), मत्स्य (मछली), मधुमक्खी।
- पशुधन प्रबंधन के पहलू:
- पशुधन का भोजन (Feeding): जानवरों को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए उचित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा जानवर की प्रजाति, उम्र और उत्पादन के चरण पर निर्भर करती है। चारे मेंRoughage (रेशा) और Concentrate (पोषक तत्वों से भरपूर) का उचित मिश्रण होना चाहिए।
- पशुधन का आश्रय (Shelter): जानवरों को आरामदायक, स्वच्छ और सुरक्षित आश्रय प्रदान करना आवश्यक है ताकि उन्हें प्रतिकूल मौसम, शिकारियों और बीमारियों से बचाया जा सके। आश्रय हवादार और उचित तापमान वाला होना चाहिए।
- पशुधन का प्रजनन (Breeding): अच्छी नस्लों के जानवरों को प्राप्त करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान (artificial insemination) शामिल हैं। नस्लों को उनकी वांछित विशेषताओं (जैसे उच्च दूध उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता) के आधार पर चुना जाता है।
- रोग नियंत्रण (Disease Control): पशुओं को बीमारियों से बचाना और बीमार होने पर उनका उचित इलाज करना आवश्यक है। इसके लिए टीकाकरण (vaccination), नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वच्छ वातावरण महत्वपूर्ण हैं।
- कुक्कुट पालन (Poultry Farming): यह अंडे और मांस के उत्पादन के लिए मुर्गियों, बत्तखों और टर्की जैसे पक्षियों का पालन है।
- अंडे और मांस उत्पादन: विभिन्न नस्लें अंडे और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं।
- प्रबंधन: उचित भोजन, स्वच्छ आवास, बीमारियों से सुरक्षा और उचित तापमान बनाए रखना आवश्यक है।
- मत्स्य पालन (Fish Farming / Pisciculture): यह भोजन के लिए मछलियों का प्रजनन, पालन और विपणन है।
- मछली के स्रोत: प्राकृतिक जल निकाय (जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र) और कृत्रिम तालाब।
- जलीय कृषि (Aquaculture): जलीय जीवों (मछली, झींगा, केकड़ा, शैवाल) का नियंत्रित वातावरण में उत्पादन।
- मत्स्य पालन के प्रकार:
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन (Inland Fisheries): तालाबों, झीलों, नदियों और नहरों में मछली पालन।
- समुद्री मत्स्य पालन (Marine Fisheries): समुद्र में मछली पकड़ना और पालन करना।
- सतत मत्स्य पालन (Sustainable Fisheries): मछली पकड़ने की ऐसी विधियों का उपयोग करना जिससे मछली की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और भविष्य के लिए मछली संसाधन बने रहें।
- मधुमक्खी पालन (Bee-keeping / Apiculture): यह शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों का पालन है।
- शहद और मोम उत्पादन: शहद एक पौष्टिक भोजन है और मोम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है।
- प्रबंधन: मधुमक्खी के छत्तों को सुरक्षित स्थान पर रखना, उन्हें बीमारियों और कीटों से बचाना, और शहद निकालने की उचित तकनीक का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियाँ परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे फसल की उपज बढ़ती है।