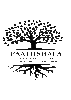अध्याय 13: हमारा पर्यावरण
- परिचय
- पर्यावरण क्या है?
- जैविक घटक
- अजैविक घटक
- पारितंत्र – इसके घटक
- परिभाषा
- जैविक घटक
- उत्पादक
- उपभोक्ता
- अपघटक
- अजैविक घटक
- खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल
- खाद्य श्रृंखला
- खाद्य जाल
- ऊर्जा का प्रवाह
- 10% का नियम
- जैविक आवर्धन
- हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव
- ओजोन परत का क्षरण
- ओजोन परत
- ओजोन परत का क्षरण
- प्रभाव
- बचाव के उपाय
- कचरा प्रबंधन
- प्रकार का कचरा
- कचरा प्रबंधन की समस्याएँ
- कचरा प्रबंधन के तरीके
- ओजोन परत का क्षरण
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
- वन और वन्यजीव
- वनों का महत्व
- वनों की कटाई
- वन्यजीवों का संरक्षण
- सतत वन प्रबंधन
- जल संसाधन
- जल का महत्व
- जल प्रदूषण
- जल संरक्षण
- कोयला और पेट्रोलियम
- वन और वन्यजीव
- सतत विकास
- सारांश
- अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु
परिचय:
यह अध्याय हमें हमारे आसपास के पर्यावरण, उसमें होने वाले परिवर्तनों और मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताता है। यह नोट्स NCERT की पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री पर आधारित हैं ताकि आपको विषय को आसानी से समझने में मदद मिल सके।
मुख्य विषय:
- पर्यावरण क्या है? (What is Environment?):
- हमारे आसपास की हर चीज, जिसमें जीवित (जैविक) और निर्जीव (अजैविक) घटक शामिल हैं, पर्यावरण कहलाती है।
- जैविक घटक (Biotic Components): सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि।
- अजैविक घटक (Abiotic Components): सभी निर्जीव चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान आदि।
- पारितंत्र – इसके घटक (Ecosystem – Its Components):
- परिभाषा: एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक इकाई बनाते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं।
- एक पारितंत्र आत्मनिर्भर हो सकता है और उसमें ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण होता है।
- घटक:
- जैविक घटक (Biotic Components):
- उत्पादक (Producers): वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया (प्रकाश संश्लेषण द्वारा)। ये पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं।
- उपभोक्ता (Consumers): वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। इन्हें विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है:
- प्राथमिक उपभोक्ता (Primary Consumers या शाकाहारी): वे जीव जो पौधों को खाते हैं (जैसे हिरण, गाय, टिड्डा)।
- द्वितीयक उपभोक्ता (Secondary Consumers या मांसाहारी): वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं (जैसे लोमड़ी, मेंढक)।
- तृतीयक उपभोक्ता (Tertiary Consumers या उच्च मांसाहारी): वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं (जैसे शेर, बाज)।
- सर्वभक्षी (Omnivores): वे जीव जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं (जैसे मनुष्य, कौआ)।
- अपघटक (Decomposers): वे सूक्ष्मजीव (जैसे बैक्टीरिया और कवक) जो मृत पौधों और जंतुओं को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। ये पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अजैविक घटक (Abiotic Components): जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान, खनिज आदि। ये जैविक घटकों के अस्तित्व और कार्य को प्रभावित करते हैं।
- जैविक घटक (Biotic Components):
- खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल (Food Chains and Food Webs):
- खाद्य श्रृंखला (Food Chain): एक सीधी श्रृंखला है जो दिखाती है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे स्थानांतरित होती है। प्रत्येक स्तर एक पोषण स्तर (Trophic Level) कहलाता है।
- उदाहरण: घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज
- पहले पोषण स्तर पर उत्पादक होते हैं, दूसरे पर प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे पर द्वितीयक उपभोक्ता और इसी तरह आगे।
- खाद्य जाल (Food Web): एक पारितंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे एक जटिल जाल बनता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। यह पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अधिक वास्तविक तस्वीर दिखाता है क्योंकि जीव अक्सर एक से अधिक प्रकार के भोजन खाते हैं।
- खाद्य श्रृंखला (Food Chain): एक सीधी श्रृंखला है जो दिखाती है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे स्थानांतरित होती है। प्रत्येक स्तर एक पोषण स्तर (Trophic Level) कहलाता है।
- ऊर्जा का प्रवाह (Flow of Energy):
- पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है।
- उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का लगभग 1% भाग भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
- जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है, तो लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुँचती है, जबकि शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है या जीव की जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग हो जाती है। इसे 10% का नियम (10% Law) कहते हैं।
- इसी कारण से खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या आमतौर पर 3-4 ही होती है, क्योंकि उच्च पोषण स्तरों पर पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है।
- ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है (उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर)।
- जैविक आवर्धन (Biological Magnification):
- कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ (जैसे कीटनाशक – DDT, भारी धातुएँ) जो पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, अपघटित नहीं होते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं।
- जैसे-जैसे ये पदार्थ एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। इसे जैविक आवर्धन कहते हैं।
- उच्च पोषण स्तरों पर जीवों में इन हानिकारक पदार्थों की सांद्रता सबसे अधिक होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव (Impact of Our Activities on the Environment):
- मानव गतिविधियाँ पर्यावरण को कई तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं:
- ओजोन परत का क्षरण (Depletion of Ozone Layer):
- ओजोन परत (Ozone Layer): यह समताप मंडल (Stratosphere) में पाई जाने वाली ओजोन (O3) गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet – UV) किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकती है।
- ओजोन परत का क्षरण: क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे रासायनिक पदार्थ (जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एयरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाते थे) वायुमंडल में पहुँचकर ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है।
- प्रभाव: ओजोन परत के क्षरण से पृथ्वी पर अधिक UV किरणें पहुँचती हैं, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना और पौधों व जलीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं।
- बचाव के उपाय: CFCs के उपयोग को कम करना और उनके विकल्पों का उपयोग करना (जैसे HCFCs)। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कई समझौते हुए हैं (जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल)।
- कचरा प्रबंधन (Waste Management):
- हमारी जीवनशैली के कारण बड़ी मात्रा में कचरा (घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, अस्पताल का कचरा आदि) उत्पन्न होता है।
- प्रकार का कचरा:
- जैव निम्नीकरणीय कचरा (Biodegradable Waste): वह कचरा जो सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है (जैसे सब्जी और फलों के छिलके, कागज)।
- अजैव निम्नीकरणीय कचरा (Non-biodegradable Waste): वह कचरा जो आसानी से विघटित नहीं होता है (जैसे प्लास्टिक, धातुएँ, कांच)।
- कचरा प्रबंधन की समस्याएँ: कचरे का ढेर लगना, प्रदूषण (वायु, जल, मिट्टी), स्वास्थ्य समस्याएँ।
- कचरा प्रबंधन के तरीके:
- कचरे को कम करना (Reduce): वस्तुओं का कम उपयोग करना।
- पुन: उपयोग करना (Reuse): वस्तुओं को बार-बार उपयोग करना।
- पुनर्चक्रण करना (Recycle): कचरे से नई उपयोगी वस्तुएँ बनाना।
- जैव निम्नीकरण (Composting): जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करना।
- भराव क्षेत्र (Landfills): कचरे को जमीन में दबाना (यह एक अस्थायी समाधान है और इससे प्रदूषण हो सकता है)।
- भस्मीकरण (Incineration): कचरे को उच्च तापमान पर जलाना (इससे वायु प्रदूषण हो सकता है)।
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन (Management of Natural Resources):
- प्राकृतिक संसाधन (जैसे वन, जल, कोयला, पेट्रोलियम) हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनका अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है।
- वन और वन्यजीव (Forests and Wildlife):
- वनों का महत्व: ऑक्सीजन उत्पादन, जल चक्र बनाए रखना, मिट्टी का कटाव रोकना, जैव विविधता बनाए रखना, आदि।
- वनों की कटाई (Deforestation): वनों को काटना। इसके कारण मृदा अपरदन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि होती है।
- वन्यजीवों का संरक्षण: जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शिकार और आवास विनाश से वन्यजीवों की संख्या कम हो रही है।
- सतत वन प्रबंधन (Sustainable Forest Management): वनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें।
- जल संसाधन (Water Resources):
- जल का महत्व: जीवन के लिए आवश्यक, कृषि और उद्योगों में उपयोग।
- जल प्रदूषण: घरेलू और औद्योगिक कचरे के कारण जल का दूषित होना।
- जल संरक्षण: जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों को साफ रखना।
- कोयला और पेट्रोलियम (Coal and Petroleum):
- ये जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन इनके जलने से वायु प्रदूषण होता है और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।
- इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत) की ओर बढ़ना आवश्यक है।
- सतत विकास (Sustainable Development):
- विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
- इसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है।
सारांश:
इस अध्याय में हमने पर्यावरण, पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, जैविक आवर्धन और मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सीखा। हमने ओजोन परत के क्षरण, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता पर भी चर्चा की। अंत में, हमने सतत विकास के महत्व को समझा जो पर्यावरण को बचाते हुए विकास करने पर जोर देता है।
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु:
- पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
- हमें अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लाकर पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए।
- सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियाँ और कानून बनाने चाहिए।