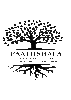अध्याय 1 – पालमपुर गाँव की कहानी
विषय वस्तु (Content):
- परिचय: पालमपुर गाँव की कहानी का एक काल्पनिक अवलोकन, मुख्य क्रियाएँ एवं सुविधाएँ।
- उत्पादन का संगठन: उत्पादन के कारक – भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी (स्थायी एवं कार्यशील), मानव पूँजी।
- पालमपुर में खेती:
- भूमि स्थिर है।
- क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? (बहुविध फसल प्रणाली, आधुनिक कृषि विधियाँ)
- क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? (भूमि की उर्वरता पर प्रभाव)
- पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है?
- श्रम की व्यवस्था कौन करेगा?
- खेतों के लिए आवश्यक पूँजी।
- अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री।
- पालमपुर गाँव में गैर-कृषि क्रियाएँ: डेयरी, लघु-स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि।
- सारांश
विस्तृत नोट्स:
1. परिचय (Introduction):
- पालमपुर गाँव: यह एक काल्पनिक गाँव है जिसके माध्यम से उत्पादन से संबंधित मूल विचारों और गाँव में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को समझाया गया है।
- मुख्य क्रिया: पालमपुर में खेती मुख्य आर्थिक क्रिया है। लगभग 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं।
- अन्य क्रियाएँ: गैर-कृषि क्रियाएँ जैसे लघु-स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि भी सीमित स्तर पर की जाती हैं।
- गाँव की अवस्थिति एवं सुविधाएँ:
- पालमपुर अपने आस-पास के गाँवों और कस्बों (जैसे रायगंज – बड़ा गाँव, शाहपुर – निकटतम कस्बा) से भली-भाँति जुड़ा हुआ है।
- प्रत्येक मौसम में यह सड़क गाँव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है।
- इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियाँ, भैंसा-बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं।
- गाँव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं।
- अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं।
- अनुसूचित जाति (दलित) के लोगों की संख्या गाँव की कुल जनसंख्या का एक तिहाई है और वे गाँव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं।
- गाँव में अधिकांश घरों में बिजली की सुविधा है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है।
- पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है।
- गाँव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है।
- इन सुविधाओं (विकसित सिंचाई प्रणाली, सड़कों का जाल, परिवहन के साधन, बिजली, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र) की तुलना अपने निकट के गाँव की सुविधाओं से की जा सकती है
-
2उत्पादन का संगठन (Organisation of Production):
उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार मुख्य चीजें आवश्यक होती हैं, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है:
- (क) भूमि (Land):
- यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसमें केवल जमीन ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज भी शामिल हैं।
- भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसकी मात्रा स्थिर होती है।
- (ख) श्रम (Labour):
- उत्पादन क्रियाओं को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है, तो कुछ में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की।
- श्रम प्रदान करने वाले या तो स्वयं किसान और उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं या फिर किराए के श्रमिक (मजदूर) हो सकते हैं।
- (ग) भौतिक पूँजी (Physical Capital):
- उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत (inputs) भौतिक पूँजी कहलाते हैं। इसके दो प्रकार हैं:
- स्थायी पूँजी (Fixed Capital): औजार, मशीन, भवन जिनका उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। उदाहरण: किसान का हल, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ट्रैक्टर आदि।
- कार्यशील पूँजी (Working Capital): कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण: बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, नकद पैसा।
- उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत (inputs) भौतिक पूँजी कहलाते हैं। इसके दो प्रकार हैं:
- (घ) मानव पूँजी (Human Capital):
- उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूँजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम (Knowledge and Enterprise) की आवश्यकता होती है। इसे आजकल मानव पूँजी कहा जाता है।
- इसमें व्यक्ति का कौशल, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव शामिल होता है जो उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर और अधिक कुशल बनाता है।
- एक उद्यमी (Entrepreneur) वह व्यक्ति होता है जो इन सभी कारकों को संगठित करके उत्पादन का जोखिम उठाता है।
-
4,पालमपुर गाँव में खेती (Farming in Palampur):
- (क) भूमि स्थिर है (Land is Fixed):
- पालमपुर गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं।
- 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, लेकिन नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
- भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यद्यपि गाँवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है।
- (ख) क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? (Is there a way to grow more from the same land?): पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। एक वर्ष में किसान एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन बढ़ाते हैं। इसके दो मुख्य तरीके हैं:
- बहुविध फसल प्रणाली (Multiple Cropping System):
-
-
- एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं।
- पालमपुर के किसान कम से कम दो मुख्य फसलें उगाते हैं; कई किसान पिछले पंद्रह-बीस वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं।
- उदाहरण: बरसात (खरीफ) के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम (रबी) में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है।
- सिंचाई व्यवस्था: पालमपुर में सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, जिसके कारण किसान एक वर्ष में तीन अलग-अलग फसलें उगा पाते हैं। पहले किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप, 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी।
-
- आधुनिक कृषि विधियाँ (Modern Farming Methods):
-
-
- 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति (Green Revolution) ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों (HYV – High Yielding Varieties) के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए।
- अधिक उपज वाले बीज (HYV): परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणामस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी।
- आवश्यकताएँ: HYV बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी।
- उपकरण: आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों का उपयोग होता है, जिसने जुताई और कटाई को तेज कर दिया।
- पालमपुर में प्रभाव: पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूँ की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गई। इससे गेहूँ के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिक मात्रा में ‘अधिशेष’ गेहूँ उपलब्ध होने लगा।
- सबसे पहले प्रयोग: भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया।
-
- (ग) क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? (Will the land sustain?):
- आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है।
- उर्वरता में कमी: रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। ये उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं।
- जल स्तर में कमी: नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमिगत जल के सतत प्रयोग से भौम जलस्तर कम हो गया है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: रासायनिक उर्वरक पानी में घुलकर नदियों और भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं।
- दीर्घकालिक खेती: कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग या जैविक खाद का प्रयोग करके भूमि की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है।
- (घ) पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? (How is land distributed among the farmers of Palampur?):
- पालमपुर में सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है।
- भूमिहीन किसान: पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात् 150 परिवार भूमिहीन हैं, जो अधिकांशतः दलित हैं।
- छोटे किसान: 240 परिवार छोटे भूमि के टुकड़ों (2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल) पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती।
- मझोले और बड़े किसान: पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है।
- यह असमान वितरण दर्शाता है कि अधिकांश छोटे किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं, जबकि बड़े किसान अधिशेष उत्पादन से लाभ कमाते हैं।
- (ङ) श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? (Who will provide the labour?): खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है।
- छोटे किसान: अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं।
- मझोले और बड़े किसान: अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों (खेत मजदूर) को किराए पर लगाते हैं।
- खेत मजदूर: ये भूमिहीन परिवारों या बहुत छोटे भूखंडों पर खेती करने वाले परिवारों से आते हैं। उन्हें किसानों द्वारा उगाई जा रही फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें नकद या वस्तु (जैसे अनाज) के रूप में मजदूरी मिलती है।
- मजदूरी: मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य (जैसे बुआई और कटाई) के लिए अलग-अलग होती है।
- रोजगार की अवधि: खेत मजदूरों को दैनिक, या किसी विशेष कृषि कार्य (जैसे कटाई) या पूरे साल के लिए काम मिल सकता है।
- कम मजदूरी और प्रतिस्पर्धा: पालमपुर में खेत मजदूरों में काम के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है। (उदाहरण: डाला एक भूमिहीन खेत मजदूर है)।
- (च) खेतों के लिए आवश्यक पूँजी (The capital needed in farming): खेती के लिए किसानों को पहले से अधिक पैसे की आवश्यकता होती है।
- छोटे किसान: अधिकांश छोटे किसानों को पूँजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। (उदाहरण: सविता की कहानी)।
- मझोले और बड़े किसान: इनकी खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूँजी की व्यवस्था कर लेते हैं। वे इस बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए या ट्रैक्टर खरीदने जैसे स्थायी पूँजी में निवेश करने या छोटे किसानों को उधार देने में करते हैं।
- (छ) अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री (Sale of surplus farm products):
- किसान उत्पादन के बाद उत्पाद का एक हिस्सा अपने परिवार के उपभोग के लिए रखते हैं और शेष (अधिशेष) को बेच देते हैं।
- छोटे किसान: छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष उत्पादन होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं।
- मझोले और बड़े किसान: यही बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। वे अधिशेष कृषि उत्पादों को पास के रायगंज के बाजार में या शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं।
- आय का उपयोग: इस आय का उपयोग वे अगले मौसम के लिए पूँजी की व्यवस्था करने, बैंक में जमा करने, या पशु, ट्रक खरीदने या दुकानें खोलने जैसे गैर-कृषि कार्यों में निवेश करने में करते हैं। (उदाहरण: तेजपाल सिंह, एक बड़ा किसान)।
- पालमपुर में गैर-कृषि क्रियाएँ (Non-farm Activities in Palampur):
पालमपुर में खेती के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाएँ भी होती हैं, जिन्हें गैर-कृषि क्रियाएँ कहते हैं। गाँव के कुल कामगारों का केवल 25% ही इन कार्यों में लगा है।
- (क) डेयरी (Dairy):
- पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा (चारा) खिलाते हैं।
- दूध को निकट के बड़े गाँव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध दूर-दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है।
- (ख) लघु-स्तरीय विनिर्माण (Small-scale Manufacturing):
- पालमपुर में भारत के शहरों और कस्बों में बड़े कारखानों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत, बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है।
- ये कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किए जाते हैं। श्रमिकों को कभी-कभार ही किराए पर लिया जाता है।
- उदाहरण: मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल को थोड़ा लाभ हो जाता है।
- (ग) दुकानदारी (Shopkeeping):
- पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार (वस्तु-विनिमय) नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएँ खरीदते हैं और उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं।
- गाँव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं।
- कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में ही छोटी दुकानें खोल ली हैं। वे खाने की चीजें भी बेचते हैं।
- उदाहरण: करीम ने गाँव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गाँव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। उसने गाँव में ही कंप्यूटर सिखाने का निर्णय लिया। उसने दो कंप्यूटर खरीदे और अपने घर के बाहर खुले में कक्षाएँ प्रारंभ कीं। हाई स्कूल के दो छात्रों ने उसके यहाँ काम करना शुरू किया।
- (घ) परिवहन: तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्रक (Transport: A Fast Developing Sector):
- पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शावाले, ताँगेवाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं।
- ये लोग वस्तुओं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं।
- पिछले कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है।
-
सारांश (Summary):
- पालमपुर गाँव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सिंचाई के विस्तार और आधुनिक कृषि विधियों (HYV बीज, रासायनिक उर्वरक) के कारण किसान उसी भूमि से अधिक उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं।
- उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी और मानव पूँजी आवश्यक कारक हैं।
- भूमि एक सीमित और स्थिर संसाधन है। इसके सतत उपयोग पर ध्यान देना आवश्यक है।
- किसानों में भूमि का वितरण असमान है, जिससे कई छोटे किसान और खेत मजदूर गरीबी में जीवन यापन करते हैं।
- छोटे किसानों को पूँजी की व्यवस्था के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जबकि बड़े किसान अपनी बचत से पूँजी जुटाते हैं।
- अधिशेष कृषि उत्पादों को बाजार में बेचा जाता है, जिससे किसानों को आय प्राप्त होती है।
- पालमपुर में डेयरी, लघु-स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन जैसी गैर-कृषि क्रियाएँ भी महत्वपूर्ण हो रही हैं, जो आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं।
भविष्य में, गाँवों में गैर-कृषि उत्पादन क्रियाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि खेती पर जनसंख्या का दबाव कम हो सके और लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके। इसके लिए पूँजी, बाजार और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी।