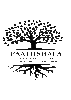अध्याय 1 – लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों?
विषय वस्तु
- परिचय: लोकतंत्र क्या है?
- लोकतंत्र की सरल परिभाषा।
- परिभाषा की आवश्यकता और विभिन्न पहलू।
- लोकतंत्र की विशेषताएँ:
- प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला।
- एक व्यक्ति-एक वोट-एक मोल।
- कानून का राज और अधिकारों का आदर।
- परिभाषा का सारांश।
- लोकतंत्र ही क्यों?
- लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क (कमियाँ)।
- लोकतंत्र के पक्ष में तर्क (गुण/महत्व)।
- लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ:
- प्रतिनिधि लोकतंत्र।
- लोकतंत्र और नागरिक।
- आदर्श लोकतंत्र बनाम वास्तविक लोकतंत्र।
- निष्कर्ष: लोकतंत्र का महत्व और भविष्य।
विस्तृत नोट्स
- परिचय: लोकतंत्र क्या है? (Introduction: What is Democracy?)
- लोकतंत्र की सरल परिभाषा (Simple Definition of Democracy):
- लोकतंत्र (Democracy) शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं।
- यह शब्द यूनानी शब्द ‘डेमोक्रेटिया’ (Demokratia) से बना है। यूनानी में ‘डेमोस’ (Demos) का अर्थ होता है ‘लोग’ और ‘क्रेटिया’ (Kratia) का अर्थ होता है ‘शासन’। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है ‘लोगों का शासन’।
- परिभाषा की आवश्यकता और विभिन्न पहलू (Need for Definition and Various Aspects):
- यह सरल परिभाषा हमें अलोकतांत्रिक सरकारों से लोकतंत्र को अलग करने में मदद करती है (जैसे राजशाही, तानाशाही)।
- लेकिन सिर्फ शासकों का चुनाव ही लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि:
- शासक कौन होने चाहिए? (क्या सभी नागरिक या कुछ विशेष लोग?)
- चुनाव किस प्रकार के होने चाहिए? (क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष?)
- कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? (क्या सभी नागरिकों को समान अधिकार हैं?)
- शासन का स्वरूप कैसा हो? (क्या चुने हुए शासक अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या कुछ बुनियादी नियमों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहकर काम करना होता है?)
- इन विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए लोकतंत्र की विशेषताओं पर गौर करना आवश्यक है।
- लोकतंत्र की विशेषताएँ (Features of Democracy):
- प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में (Major decisions by elected leaders):
- सिद्धांत: लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।
- उदाहरण (नकारात्मक):
- पाकिस्तान (परवेज मुशर्रफ): अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट के जरिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को ‘मुख्य कार्यकारी’ घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराके अपना कार्यकाल पाँच साल के लिए बढ़वा लिया (यह जनमत संग्रह धोखाधड़ी और गड़बड़ियों पर आधारित था)। अगस्त 2002 में उन्होंने ‘लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर’ के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार, राष्ट्रपति नेशनल और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। अतः इसे वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास नहीं थी।
- निष्कर्ष: लोकतंत्र में असली ताकत उन नेताओं के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है, न कि किसी बाहरी शक्ति (जैसे सेना) या अ-निर्वाचित व्यक्ति के पास।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला (Free and fair electoral competition):
- सिद्धांत: लोकतंत्र सिर्फ चुनाव करा देना भर नहीं है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से आयोजित होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार-जीत के समान अवसर हों।
- उदाहरण (नकारात्मक):
- चीन: चीन की संसद (क्वांगुओ रेममिन दाइबियाओ दाहुई – राष्ट्रीय जन संसद) के लिए प्रति पाँच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यहाँ चुनाव तो होते हैं लेकिन लोगों के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, इसलिए इसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता।
- मैक्सिको: मैक्सिको में 1930 में आजाद होने के बाद से हर छह वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन् 2000 तक हर चुनाव में ‘इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी’ (पी.आर.आई.) नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पी.आर.आई. कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र-छात्राओं के माँ-बाप से पी.आर.आई. के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब-तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केन्द्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। पी.आर.आई. अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी।
- निष्कर्ष: लोकतंत्र में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए और चुनाव इतने निष्पक्ष हों कि शासक दल के हारने की भी संभावना हो।
- एक व्यक्ति-एक वोट-एक मोल (One person, one vote, one value):
- सिद्धांत: लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य समान होना चाहिए। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार से जुड़ा है।
- उदाहरण (नकारात्मक):
- सऊदी अरब (2015 तक): 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था।
- एस्टोनिया: एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है।
- फिजी: फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है।
- निष्कर्ष: लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए, सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए।
- कानून का राज और अधिकारों का आदर (Rule of law and respect for rights):
- सिद्धांत: एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ चुनाव जीत जाने के कारण मनमानी नहीं कर सकती। उसे कुछ बुनियादी नियमों और नागरिक अधिकारों का सम्मान करना होता है। सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है।
- उदाहरण (नकारात्मक):
- जिम्बाब्वे: जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर ‘जानू-पीएफ’ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता-संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे (2017 तक)। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू-पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी तथा उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला।
- निष्कर्ष: एक लोकतांत्रिक सरकार केवल बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लेती। उसे अल्पमत के विचारों का भी सम्मान करना होता है। नागरिकों को सोचने की, अपनी राय जाहिर करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियाँ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार को नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करना चाहिए और कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए और उसके आदेशों का पालन होना चाहिए।
- परिभाषा का सारांश (Summary of Definition):
उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर लोकतंत्र की एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है:
“लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें:
- लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं;
- चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकें;
- यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों; और
- इस चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है।”
- लोकतंत्र ही क्यों? (Why Democracy?)
लोकतंत्र शासन का सबसे अच्छा स्वरूप क्यों माना जाता है? इसे समझने के लिए इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर विचार करना होगा।
- लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क (Arguments against Democracy – कमियाँ):
- अस्थिरता (Instability): लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। बार-बार नीतियां बदलने से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है।
- नैतिकता का अभाव (Lack of Morality): लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल चलता है, यहाँ नैतिकता की कोई खास जगह नहीं होती। नेता चुनाव जीतने के लिए कई बार गलत हथकंडे अपनाते हैं।
- फैसलों में देरी (Delay in Decision Making): लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हर फैसले में देरी होती है।
- खराब फैसले (Bad Decisions): चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का ठीक-ठीक पता नहीं होता, इसके चलते कई बार खराब फैसले हो जाते हैं।
- भ्रष्टाचार की संभावना (Possibility of Corruption): लोकतंत्र में चुनावी प्रणाली खर्चीली होती है, और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं।
- सामान्य लोगों को समझ का अभाव (Lack of Understanding in Common People): आम लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए।
- बहुमत का शासन (Rule of Majority): लोकतंत्र में अक्सर बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अल्पमत के हितों की अनदेखी हो सकती है।
- लोकतंत्र के पक्ष में तर्क (Arguments for Democracy – गुण/महत्व):
- अधिक जवाबदेह शासन (More Accountable Form of Government): लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती हैं क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है और अगले चुनाव में हार का डर रहता है। गैर-लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर काम करने की संभावना ज्यादा होती है।
- उदाहरण: भारत और चीन में 1958-61 के दौरान पड़े अकाल का तुलनात्मक अध्ययन। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जिस तरह अकाल का सामना किया, वैसा चीन की सरकार नहीं कर पाई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण ऐसा हुआ। भारत में स्वतंत्र मीडिया, विपक्षी दल और सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता होने के कारण सरकार पर खाद्य सुरक्षा के मामले में कार्रवाई करने का दबाव बना। चीन में यह व्यवस्था नहीं थी।
- बेहतर निर्णय लेने की संभावना (Improved Quality of Decision Making): लोकतंत्र में व्यापक चर्चा और बहस के बाद फैसले लिए जाते हैं। अनेक लोगों की सोच और सलाह शामिल होने से गलतियों की गुंजाइश कम होती है। भले ही इसमें समय अधिक लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श करके फैसले लेने से बेहतर परिणाम आते हैं।
- मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है (Provides a Method to Deal with Differences and Conflicts): भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश में विभिन्न भाषा, धर्म और जाति के लोग रहते हैं। लोकतंत्र ही ऐसी व्यवस्था है जो इन विभिन्न समूहों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से टकरावों को सुलझा सकती है और सबको साथ लेकर चल सकती है। लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता या स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं।
- नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है (Enhances the Dignity of Citizens): लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सबसे गरीब और सबसे कम पढ़े-लिखे को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े-लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं। जब वे गलतियाँ करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं।
- गलतियों को सुधारने का अवसर (Allows Room to Correct Mistakes): लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गलतियाँ नहीं हो सकतीं। लेकिन इसमें यह सुविधा है कि इन गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश होती है और फिर उनमें सुधार करने का भी अवसर मिलता है। या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है।
- नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा (Political Education to Citizens): लोकतंत्र नागरिकों को राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागरूक बनाता है। चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक बहसें और अधिकारों की चर्चा से नागरिकों में राजनीतिक समझ विकसित होती है।
- अधिक जवाबदेह शासन (More Accountable Form of Government): लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती हैं क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है और अगले चुनाव में हार का डर रहता है। गैर-लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर काम करने की संभावना ज्यादा होती है।
निष्कर्ष (तर्कों का): लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादुई छड़ी नहीं है। इसने हमारे देश या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी या अन्य समस्याओं को खत्म नहीं किया है। लेकिन शासन के अन्य स्वरूपों की तुलना में यह निश्चित रूप से बेहतर है क्योंकि यह लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में बेहतर है, यह बेहतर फैसले लेने की संभावना बढ़ाता है, और यह नागरिकों का सम्मान करता है।
- लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ (Broader Meaning of Democracy):
इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा।
- प्रतिनिधि लोकतंत्र (Representative Democracy):
- आधुनिक दुनिया में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप ‘प्रतिनिधि लोकतंत्र’ है। इसमें सभी लोग सीधे शासन नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सामूहिक रूप से फैसले लेते हैं।
- यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि:
- आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता।
- अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता।
- लोकतंत्र और नागरिक (Democracy and Citizens):
- एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।
- इसके लिए नागरिकों को जागरूक, शिक्षित और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत होना आवश्यक है।
- सिर्फ वोट देने तक ही नागरिक की भूमिका सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों पर नजर रखना, सवाल उठाना और सार्वजनिक बहसों में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है।
- आदर्श लोकतंत्र बनाम वास्तविक लोकतंत्र (Ideal Democracy vs. Real Democracy):
- कोई भी देश शायद ही लोकतंत्र के सभी आदर्शों पर खरा उतरता हो। हम जिन देशों को आज लोकतांत्रिक कहते हैं, वे भी पूरी तरह आदर्श लोकतंत्र नहीं हैं।
- लोकतंत्र की हमारी समझ हमें बार-बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है।
- इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है।
- इसका मतलब यह है कि किसी भी देश में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की संभावनाएँ हमेशा बनी रहती हैं।
- निष्कर्ष: लोकतंत्र का महत्व और भविष्य (Conclusion: Importance and Future of Democracy):
- लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक सिद्धांत, एक आदर्श और जीवन का एक तरीका भी है।
- दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ कम नहीं हैं। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सतर्कता पर निर्भर करती है।
- लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसके मूल्यों और सिद्धांतों को कितना आत्मसात करते हैं और इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए कितने प्रयास करते हैं।
सहायक सामग्री आधारित अतिरिक्त बिंदु (Points from Supporting Material):
- गैर-लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण:
- राजशाही: शासक वंशानुगत होते हैं (जैसे सऊदी अरब, भूटान – हालांकि भूटान अब संवैधानिक राजतंत्र है)।
- तानाशाही/सैनिक शासन: एक व्यक्ति या एक समूह का शासन जो बलपूर्वक सत्ता में आता है (जैसे म्यांमार में सैनिक शासन, पहले चिली में पिनोशे का शासन)।
- एकदलीय शासन: केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति होती है (जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी)।
- लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक शर्तें:
- नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी।
- कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका।
- स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया।
- सक्रिय और जागरूक नागरिक समाज।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण।
- लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल: प्रत्यक्ष लोकतंत्र (जैसे प्राचीन एथेंस या कुछ स्विस कैंटनों में) और अप्रत्यक्ष/प्रतिनिधि लोकतंत्र। आज के विशाल राष्ट्र-राज्यों में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही व्यवहार्य है।
- लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व।