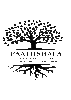अध्याय 3 – अपवाह
विषय वस्तु (Content):
- अपवाह की संकल्पना: अर्थ एवं विभिन्न अपवाह प्रतिरूप
- भारत में अपवाह तंत्र: हिमालय की नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ
- हिमालय की नदियाँ:
- सिंधु नदी तंत्र
- गंगा नदी तंत्र
- ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र
- प्रायद्वीपीय नदियाँ:
- नर्मदा द्रोणी
- तापी द्रोणी
- गोदावरी द्रोणी
- महानदी द्रोणी
- कृष्णा द्रोणी
- कावेरी द्रोणी
- झीलें: प्रकार एवं महत्व
- नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व
- नदी प्रदूषण एवं संरक्षण के उपाय
विस्तृत नोट्स:
- अपवाह की संकल्पना (Concept of Drainage):
- अपवाह (Drainage): किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या “अपवाह” शब्द से की जाती है। यह एक निर्धारित मार्ग (वाहिकाओं) के माध्यम से जल के प्रवाह को दर्शाता है। ये वाहिकाएँ मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं।
- अपवाह द्रोणी (Drainage Basin): एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे “अपवाह द्रोणी” कहते हैं। कोई भी ऊँचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, इसे “जल विभाजक” (Water Divide) कहा जाता है।
- उदाहरण के लिए, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है।
- अपवाह प्रतिरूप (Drainage Patterns): एक अपवाह क्षेत्र में नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यह भू-भाग की ढाल, चट्टानों की संरचना तथा जलवायु संबंधी अवस्थाओं पर निर्भर करता है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित हैं:
- द्रुमाकृतिक प्रतिरूप (Dendritic Pattern): जब नदी की धाराएँ उस स्थान के भू-स्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं और मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाई देती हैं। उदाहरण: उत्तरी मैदान की नदियाँ।
- जालीनुमा प्रतिरूप (Trellis Pattern): जब नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं। यह कठोर तथा मुलायम चट्टानों वाले क्षेत्रों में विकसित होता है।
- आयताकार प्रतिरूप (Rectangular Pattern): यह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भू-भाग पर विकसित होता है, जहाँ नदियाँ संधियों के सहारे बहती हैं और समकोण पर मुड़ती हैं।
- अरीय प्रतिरूप (Radial Pattern): जब नदियाँ किसी केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। उदाहरण: अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ (नर्मदा, सोन)।
- भारत में अपवाह तंत्र (Drainage Systems in India):
भारतीय नदी तंत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है:
- (क) हिमालय की नदियाँ (Himalayan Rivers):
- ये नदियाँ बारहमासी होती हैं, अर्थात् इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊँचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है।
- ये नदियाँ अपने उद्गम स्थान से समुद्र तक लंबे मार्ग तय करती हैं।
- ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं।
- मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं।
- (ख) प्रायद्वीपीय नदियाँ (Peninsular Rivers):
- ये नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है।
- हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा ये छिछली होती हैं।
- इनमें से अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। कुछ नदियाँ मध्य उच्चभूमि से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं।
- हिमालय की नदियाँ (Himalayan Rivers):
सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को “नदी तंत्र” (River System) कहा जाता है।
- सिंधु नदी तंत्र (Indus River System):
- उद्गम: तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट।
- प्रवाह दिशा: पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है।
- सहायक नदियाँ: जास्कर, नूबरा, श्योक तथा हुंजा (कश्मीर क्षेत्र में)। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं।
- कुल लंबाई: लगभग 2,900 किलोमीटर। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है।
- अपवाह क्षेत्र: इसका एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है।
- सिंधु जल समझौता (1960): भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20 प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है।
- समुद्र में मिलन: अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है।
- गंगा नदी तंत्र (Ganga River System):
- उद्गम: गंगा की मुख्य धारा ‘भागीरथी’ गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
- सहायक नदियाँ:
- हिमालय से निकलने वाली: यमुना (गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिलती है), घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियाँ बाढ़ के कारण व्यापक जन-धन हानि पहुँचाती हैं, विशेषकर कोसी नदी जिसे ‘बिहार का शोक’ भी कहा जाता है।
- प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली: चंबल, बेतवा, सोन। ये अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम होती है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है।
- प्रवाह दिशा एवं विस्तार: बाएँ तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बँट जाती है:
- भागीरथी-हुगली: एक वितरिका, दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टाई मैदानों से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- मुख्य धारा: दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले ‘मेघना’ के नाम से जानी जाती हैं।
- सुंदरवन डेल्टा: गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहत् नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को ‘सुंदरवन डेल्टा’ के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं।
- कुल लंबाई: लगभग 2,500 किलोमीटर से अधिक।
- अंबाला नगर: सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल-विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1,800 कि.मी. है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। अर्थात् प्रति 6 कि.मी. की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े-बड़े विसर्प बन जाते हैं।
- ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र (Brahmaputra River System):
- उद्गम: तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है।
- तिब्बत में नाम: ‘सांगपो’ (अर्थात् शोधक)। यहाँ इसमें जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है।
- भारत में प्रवेश: यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर (7,757 मीटर) के पास पहुँचकर यह अंग्रेजी के ‘यू’ (U) अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे ‘दिहांग’ के नाम से जाना जाता है।
- सहायक नदियाँ (भारत में): दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं।
- असम में स्वरूप: ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुंफित नदी (braided river) का निर्माण करती है और बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ‘माजुली’ ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है।
- वर्षा ऋतु में: प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुँचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह ऊँची हो जाती है और यह बार-बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है।
- बांग्लादेश में नाम: जमुना। यहाँ यह गंगा (पद्मा) से मिलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है।
- प्रायद्वीपीय नदियाँ (Peninsular Rivers):
प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे- महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएँ हैं। नर्मदा एवं तापी, दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनदमुख (Estuary) का निर्माण करती हैं।
- नर्मदा द्रोणी (Narmada Basin):
- उद्गम: मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट।
- प्रवाह दिशा: यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है।
- विशेषताएँ: समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ ‘धुँआधार प्रपात’ का निर्माण करती है।
- सहायक नदियाँ: बहुत छोटी हैं, अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं।
- अपवाह क्षेत्र: मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है।
- नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए: ‘नमामि देवि नर्मदे’ नाम की योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।
- समुद्र में मिलन: अरब सागर।
- तापी द्रोणी (Tapi Basin):
- उद्गम: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से।
- प्रवाह दिशा: यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है।
- अपवाह क्षेत्र: मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में।
- तटीय मैदान: अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुझ्झा तथा पेरियार हैं।
- समुद्र में मिलन: अरब सागर।
- गोदावरी द्रोणी (Godavari Basin):
- उद्गम: महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से।
- लंबाई: लगभग 1,500 किलोमीटर। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है।
- अपवाह क्षेत्र: यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र (लगभग 50% भाग), मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- सहायक नदियाँ: पूर्णा, वर्धा, प्रान्हिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीन सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं।
- ‘दक्षिण गंगा’: बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे ‘दक्षिण गंगा’ के नाम से भी जाना जाता है।
- समुद्र में मिलन: बंगाल की खाड़ी।
- महानदी द्रोणी (Mahanadi Basin):
- उद्गम: छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से।
- प्रवाह दिशा: ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- लंबाई: 860 किलोमीटर।
- अपवाह क्षेत्र: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा।
- कृष्णा द्रोणी (Krishna Basin):
- उद्गम: महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर।
- लंबाई: लगभग 1,400 किलोमीटर।
- सहायक नदियाँ: तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा।
- अपवाह क्षेत्र: महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश।
- समुद्र में मिलन: बंगाल की खाड़ी।
- कावेरी द्रोणी (Kaveri Basin):
- उद्गम: पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से।
- प्रवाह दिशा: तमिलनाडु में कुड्डालूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- लंबाई: 760 किलोमीटर।
- सहायक नदियाँ: अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी।
- अपवाह क्षेत्र: कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु।
- विशेषता: यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है (मानसून और लौटते मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है)। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, इसे शिवसमुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत् मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है।
- समुद्र में मिलन: बंगाल की खाड़ी।
इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे – दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा।
- झीलें (Lakes):
पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं।
- मीठे पानी की झीलें: अधिकतर हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में, ये तब बनीं जब हिमानियों ने या कोई गहरी बेसिन बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बँध गए।
- उदाहरण: जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील (भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील), डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बारापानी।
- खारे पानी की झीलें:
- उदाहरण: राजस्थान की सांभर झील (यह एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है)।
- मानव निर्मित झीलें: जल विद्युत् उत्पादन के लिए नदियों पर बाँध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है।
- उदाहरण: गुरु गोबिंद सागर (भाखड़ा-नंगल परियोजना)।
- अन्य प्रकार की झीलें:
- विसर्प झीलें (गोखुर झीलें): बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती हैं।
- लैगून: स्पिट तथा बार (रोधिका) तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। उदाहरण: चिल्का झील (ओडिशा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील), पुलिकट झील तथा कोलेरू झील।
- झीलों का महत्व:
- नदी के बहाव को सुचारु बनाने में सहायक।
- अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं।
- सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करती हैं।
- जल विद्युत् उत्पादन में सहायक।
- आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं।
- जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं।
- पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और मनोरंजन प्रदान करती हैं।
- मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण।
- नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व (Role of Rivers in the Economy):
नदियाँ मानव इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है।
- प्राचीन काल से महत्व: नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ (जैसे सिंधु घाटी सभ्यता)।
- सिंचाई: भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत।
- नौसंचालन: जल परिवहन का सस्ता माध्यम प्रदान करती हैं।
- जल विद्युत् निर्माण: ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत।
- घरेलू उपयोग: पीने, नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए जल उपलब्ध कराती हैं।
- उद्योगों के लिए जल: अनेक उद्योगों को जल की आवश्यकता होती है।
- मत्स्य पालन: आजीविका का साधन।
- पर्यटन एवं मनोरंजन: नदियों के किनारे सुंदर पर्यटन स्थल विकसित होते हैं।
- नदी प्रदूषण एवं संरक्षण के उपाय (River Pollution and Conservation Measures):
- नदी प्रदूषण के कारण:
- घरेलू अपशिष्ट: शहरों और कस्बों से निकलने वाला अशोधित वाहित मल।
- औद्योगिक अपशिष्ट: उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ एवं कचरा।
- कृषि रसायन: उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग।
- धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ: मूर्तियों का विसर्जन, शवों का प्रवाह आदि।
- ठोस कचरा: प्लास्टिक और अन्य अजैविक कचरे का नदियों में फेंका जाना।
- नदी प्रदूषण के दुष्प्रभाव:
- मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव (जल जनित बीमारियाँ)।
- जलीय जीवों पर संकट।
- पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन।
- पीने योग्य पानी की कमी।
- मिट्टी की उर्वरता में कमी (प्रदूषित जल से सिंचाई)।
- नदी संरक्षण के उपाय:
- अपशिष्ट जल का शोधन: शहरों और उद्योगों के अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ने से पहले शोधित करना।
- औद्योगिक नियमों का सख्ती से पालन: उद्योगों को प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करना।
- जैविक खेती को बढ़ावा: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कम करना।
- जागरूकता अभियान: लोगों को नदी प्रदूषण के खतरों और संरक्षण के उपायों के बारे में जागरूक करना।
- कानूनी प्रावधान: नदी प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई।
- वृक्षारोपण: नदियों के किनारों पर वृक्षारोपण करने से मिट्टी का कटाव रुकता है और जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- नदी सफाई अभियान: विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे नदी सफाई अभियानों में सक्रिय भागीदारी। उदाहरण: गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे परियोजना।
- ठोस कचरा प्रबंधन: कचरे को नदियों में फेंकने से रोकना और उचित निपटान सुनिश्चित करना।