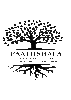अध्याय 5 – आधुनिक विश्व में चरवाहे
विषय वस्तु
- परिचय: घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही
- चरवाहे कौन हैं? उनकी जीवन शैली।
- घुमंतूपन के कारण और महत्व।
- पहाड़ों में चरवाहे:
- गुज्जर बकरवाल (जम्मू और कश्मीर) – मौसमी चक्र, चरागाहों की खोज।
- गद्दी (हिमाचल प्रदेश) – मौसमी चक्र, चरागाहों की खोज।
- भोटिया, शेरपा और किन्नौरी (उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल) – मौसमी चक्र।
- पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे:
- धंगर (महाराष्ट्र) – मौसमी चक्र, विभिन्न व्यवसायों के साथ संबंध।
- गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश) – पशुपालन और अन्य कार्य।
- राइका (राजस्थान) – ऊँट और भेड़/बकरी पालक, वर्षा पर निर्भरता।
- बंजारे (उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र) – लंबी दूरी के व्यापारी और चरवाहे।
- औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन:
- चरागाहों का सिमटना:
- कृषि भूमि में परिवर्तन।
- वन कानून और आरक्षित वन।
- “अपराधी जनजाति” अधिनियम।
- करों का बोझ।
- आवाजाही पर प्रतिबंध।
- व्यापार पर प्रभाव।
- चरागाहों का सिमटना:
- चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया?
- जानवरों की संख्या कम करना।
- नए चरागाहों की खोज।
- कुछ ने खेती अपनाई, कुछ मजदूर बन गए।
- अधिकारों के लिए संघर्ष (सीमित)।
- अफ्रीका में चरवाहा जीवन (तुलनात्मक अध्ययन):
- अफ्रीका में चरवाहों की विशाल आबादी।
- पूर्वी अफ्रीका के प्रमुख चरवाहा समुदाय (उदा. मसाई)।
- औपनिवेशिक काल में अफ्रीका में चरवाहों पर प्रभाव:
- भूमि का बँटवारा और चरागाहों का छिन जाना (मसाईलैंड का उदाहरण)।
- आरक्षित क्षेत्र और आवाजाही पर रोक।
- सूखे का प्रभाव और संसाधनों पर बढ़ता दबाव।
- सरदार और कबीलों पर प्रभाव।
- बदलावों का सामना करने के तरीके।
- निष्कर्ष: आधुनिक विश्व में चरवाहों का स्थान और भविष्य।
विस्तृत नोट्स
- परिचय: घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही (Introduction: Nomadic Pastoralists and their Movement):
- चरवाहे कौन हैं? (Who are Pastoralists?):
- चरवाहे वे लोग होते हैं जिनकी आजीविका मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर करती है। वे दूध, मांस, ऊन, खाल आदि के लिए मवेशी (गाय, बैल), भेड़, बकरी, ऊँट, याक जैसे जानवर पालते हैं।
- इनकी जीवन शैली जानवरों की ज़रूरतों, विशेषकर चारे और पानी की उपलब्धता, के इर्द-गिर्द घूमती है।
- घुमंतूपन के कारण और महत्व (Reasons and Significance of Nomadism):
- चारे और पानी की तलाश: सबसे मुख्य कारण जानवरों के लिए नए चरागाहों और पानी के स्रोतों की निरंतर खोज है। जब एक स्थान पर चारा खत्म हो जाता है या पानी सूख जाता है, तो वे अपने झुंडों के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
- मौसमी बदलाव: कई चरवाहा समुदाय मौसम के अनुसार अपनी आवाजाही का चक्र तय करते हैं। गर्मियों में वे ठंडे ऊँचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं और सर्दियों में वापस निचले गर्म इलाकों में आ जाते हैं।
- भूमि की उर्वरता बनाए रखना: एक ही स्थान पर लगातार चराई से भूमि बंजर हो सकती है। घुमंतूपन से भूमि को प्राकृतिक रूप से अपनी उर्वरता पुनः प्राप्त करने का समय मिल जाता है।
- व्यापार और विनिमय: घुमंतू चरवाहे अक्सर अपने पशु उत्पादों (जैसे घी, ऊन) का अनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ विनिमय या व्यापार भी करते हैं।
- पारंपरिक ज्ञान: उनके पास मौसम, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, पशुओं की बीमारियों और उनके इलाज का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है।
- पहाड़ों में चरवाहे (Pastoralists in the Mountains):
- गुज्जर बकरवाल (Jammu and Kashmir – Gujjar Bakarwals):
- ये जम्मू और कश्मीर के प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं जो मुख्यतः भेड़-बकरियाँ पालते हैं।
- मौसमी चक्र:
- सर्दियाँ: वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने झुंडों को चराते हैं, जहाँ सूखी झाड़ीदार वनस्पति मिलती है।
- गर्मियाँ (अप्रैल अंत तक): बर्फ पिघलने के साथ वे उत्तर की ओर ऊँचे पहाड़ी चरागाहों (जिन्हें ‘मर्ग’ कहा जाता है) की ओर अपनी यात्रा (काफिला) शुरू करते हैं। पीर पंजाल के दर्रों को पार करके वे कश्मीर घाटी में पहुँचते हैं।
- पतझड़ (सितंबर अंत तक): बर्फबारी शुरू होने से पहले वे वापस शिवालिक की पहाड़ियों की ओर लौटना शुरू कर देते हैं।
- इनका जीवन पूरी तरह से इन मौसमी आवाजाही पर निर्भर करता है।
- गद्दी (Himachal Pradesh – Gaddis):
- ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं, जो भेड़-बकरियाँ पालते हैं।
- मौसमी चक्र: इनका भी मौसमी चक्र गुज्जर बकरवालों जैसा ही होता है।
- सर्दियाँ: शिवालिक की निचली पहाड़ियों में।
- गर्मियाँ (अप्रैल में): उत्तर की ओर लाहौल और स्पीति के ऊँचे चरागाहों में। कई गद्दी किसान भी हैं, जो एक जगह रुककर बुआई करते हैं और फिर झुंड लेकर चरागाहों में चले जाते हैं, फसल कटाई के समय लौटते हैं।
- पतझड़ (सितंबर में): वापस शिवालिक की ओर।
- भोटिया, शेरपा और किन्नौरी (Uttarakhand, Sikkim, Himachal – Bhotiyas, Sherpas, and Kinnauris):
- ये हिमालय के अन्य चरवाहा समुदाय हैं, जो इसी तरह के मौसमी चक्र का पालन करते हैं।
- वे गर्मियों में ‘बुग्याल’ (ऊँचे अल्पाइन चरागाह) में चले जाते हैं और सर्दियों में तलहटी के जंगलों में लौट आते हैं।
- इनमें से कई समुदाय व्यापार भी करते थे, खासकर तिब्बत के साथ (औपनिवेशिक काल से पहले)।
- पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे (Pastoralists on Plateaus, Plains, and Deserts):
- धंगर (Maharashtra – Dhangars):
- ये महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, जो मुख्यतः भेड़ें पालते हैं, कुछ कंबल भी बुनते हैं और कुछ भैंसें भी पालते हैं।
- मौसमी चक्र और अनुकूलन:
- मानसून (मध्य जून से अक्टूबर): वे मध्य महाराष्ट्र के पठारी इलाकों में रहते हैं, जहाँ इस समय जानवरों के लिए पर्याप्त चारा होता है। यह क्षेत्र कम वर्षा वाला और मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है, यहाँ मुख्यतः बाजरा जैसी सूखी फसलें उगाई जाती हैं।
- अक्टूबर के बाद (सूखा मौसम): चारे और पानी की कमी होने पर वे पश्चिम की ओर कोंकण क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं।
- कोंकण में: कोंकण एक उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। यहाँ के किसान खरीफ की फसल (चावल) काटने के बाद अपने खेतों को रबी की फसल के लिए तैयार करते हैं। धंगर चरवाहों का यहाँ स्वागत किया जाता है क्योंकि उनके जानवर खेतों में चरकर खाद (मलमूत्र) प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। धंगर किसानों से चावल और अन्य अनाज लेते हैं।
- मानसून की शुरुआत से पहले: वे वापस अपने पठारी इलाकों में लौट जाते हैं, क्योंकि कोंकण में भारी वर्षा भेड़ें सहन नहीं कर पातीं।
- गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा (Karnataka and Andhra Pradesh – Gollas, Kurumas, and Kurubas):
- ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चरवाहा समुदाय हैं।
- गोल्ला समुदाय गाय-भैंस पालते थे।
- कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़-बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे।
- वे जंगलों और छोटे खेतों के आस-पास रहते थे। वे जानवरों की देखभाल के साथ-साथ छोटे-मोटे शिकार और खेती भी करते थे।
- इनकी आवाजाही पहाड़ों के चरवाहों की तरह ठंड और बर्फ से तय नहीं होती थी, बल्कि बारिश और सूखे के मौसम के बदलने से तय होती थी। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की ओर चले जाते थे और बारिश शुरू होने पर वापस पठारी क्षेत्रों में लौट आते थे।
- राइका (Rajasthan – Raikas):
- ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं।
- पशुधन:
- एक वर्ग ऊँट पालता था (मारू राइका)।
- दूसरा वर्ग भेड़-बकरियाँ पालता था।
- वर्षा पर निर्भरता: रेगिस्तान में वर्षा अनिश्चित और बहुत कम होती है, इसलिए खेती भी अस्थिर होती है। फसलें अक्सर खराब हो जाती हैं।
- आवाजाही: मानसून के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइका अपने गाँवों में रहते थे जहाँ चारा उपलब्ध होता था। अक्टूबर आते-आते ये चरागाह सूखने लगते थे। नतीजतन, वे नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की ओर निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे।
- बंजारे (Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra – Banjaras):
- ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते थे।
- ये लंबी दूरी तक जाने वाले लोग थे। वे अच्छे चरागाहों की तलाश में अपने जानवरों के साथ दूर-दूर तक जाते थे।
- वे रास्ते में गाँवों को अनाज और चारा बेचते थे। जहाँ भी जाते थे, वहाँ से खेतीहरों के लिए जानवर (बैल आदि) भी ले जाते थे और बदले में या नकद में अनाज और अन्य वस्तुएँ प्राप्त करते थे।
- औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन (Colonial Rule and the Life of Pastoralists):
औपनिवेशिक शासन (ब्रिटिश राज) के दौरान चरवाहों के जीवन में नाटकीय बदलाव आए। उनकी आवाजाही और चरागाहों पर गंभीर असर पड़ा।
- चरागाहों का सिमटना (Shrinking of Pastures):
- कृषि भूमि में परिवर्तन: अंग्रेज सरकार अधिक से अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाना चाहती थी ताकि वह लगान और कृषि उत्पादों (जैसे जूट, कपास, गेहूं) से अपनी आय बढ़ा सके। वे चरागाहों को बंजर भूमि मानते थे जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता।
- “परती भूमि नियमावली” (Wasteland Rules) लागू की गई, जिसके तहत गैर-खेतिहर भूमि को कब्जे में लेकर कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपा जाने लगा, जिन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार चरागाह कृषि भूमि में बदलने लगे।
- वन कानून और आरक्षित वन (Forest Acts and Reserved Forests):
- उन्नीसवीं सदी के मध्य तक विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। इन कानूनों के द्वारा कुछ जंगलों को ‘आरक्षित’ (Reserved) घोषित कर दिया गया जहाँ से व्यावसायिक रूप से मूल्यवान लकड़ी (जैसे देवदार, साल) मिलती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई।
- कुछ जंगलों को ‘संरक्षित’ (Protected) घोषित किया गया, जहाँ चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी कई तरह के अंकुश लगा दिए गए। उन्हें परमिट लेना पड़ता था और जंगल में बिताए जाने वाले दिनों की सीमा तय कर दी गई।
- वन अधिकारियों को शक की नजर से देखा जाता था और वे चरवाहों को जंगल में प्रवेश करने के लिए रिश्वत लेते थे।
- “अपराधी जनजाति” अधिनियम (Criminal Tribes Act):
- 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने ‘अपराधी जनजाति अधिनियम’ पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को ‘अपराधी’ समुदायों की सूची में रख दिया गया।
- उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया।
- इस कानून के लागू होते ही ऐसे समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाँवों/बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर निरंतर नजर रखती थी।
- कृषि भूमि में परिवर्तन: अंग्रेज सरकार अधिक से अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाना चाहती थी ताकि वह लगान और कृषि उत्पादों (जैसे जूट, कपास, गेहूं) से अपनी आय बढ़ा सके। वे चरागाहों को बंजर भूमि मानते थे जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता।
- करों का बोझ (Burden of Taxes):
- अंग्रेज सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए हर संभव स्रोत पर कर लगाना चाहती थी।
- उन्होंने जमीन, नहर के पानी, नमक, व्यापारिक वस्तुओं और यहाँ तक कि जानवरों पर भी कर लगा दिया।
- चरवाहों से प्रति जानवर कर वसूला जाने लगा। कर वसूली का काम ठेकेदारों को सौंपा जाता था, जो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए चरवाहों से मनमाना कर वसूलते थे।
- 1850 के दशक से कर वसूली का काम सीधे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। चरवाहों को जंगल में प्रवेश के लिए परमिट लेना होता था और प्रति जानवर कर देना पड़ता था।
- आवाजाही पर प्रतिबंध (Restrictions on Movement):
- वन कानूनों और चरागाहों के कृषि भूमि में बदलने से चरवाहों की आवाजाही के रास्ते और चरागाह सीमित हो गए।
- उन्हें उन इलाकों में जाने से रोक दिया गया जहाँ वे पीढ़ियों से जाते आ रहे थे।
- व्यापार पर प्रभाव (Impact on Trade):
- आवाजाही पर प्रतिबंध और करों के बोझ से उनके व्यापारिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? (How did Pastoralists Cope with these Changes?):
औपनिवेशिक काल में आए इन नकारात्मक बदलावों का सामना करने के लिए चरवाहों ने विभिन्न तरीके अपनाए:
- जानवरों की संख्या कम करना: जब चरागाह कम होने लगे और जानवरों को चराना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी।
- नए चरागाहों की खोज: कुछ चरवाहों ने पुराने चरागाहों के छिन जाने पर नए चरागाहों की तलाश शुरू की। उदाहरण के लिए, राजस्थान के राइका समुदाय सिंध (अब पाकिस्तान का हिस्सा) और हरियाणा जैसे नए इलाकों में जाने लगे।
- जीवन शैली में बदलाव:
- कुछ अमीर चरवाहों ने जमीन खरीदकर एक जगह बसकर खेती करना शुरू कर दिया।
- कुछ छोटे और गरीब चरवाहे कर्ज लेकर या अन्य तरीकों से दिन काटने लगे। कई खेत मजदूर बन गए या कस्बों और शहरों में छोटे-मोटे काम करने लगे।
- अधिकारों के लिए संघर्ष (Limited Struggle for Rights):
- हालांकि बड़े पैमाने पर संगठित विद्रोह कम हुए, फिर भी चरवाहों ने समय-समय पर सरकारी नियमों का विरोध किया, कभी-कभी प्रतिबंधित जंगलों में जबरन घुसकर या कर देने से इनकार करके। लेकिन ये प्रयास सीमित और बिखरे हुए थे।
- कुछ चरवाहों ने सरकार से रियायतों और मदद की अपील भी की।
- अफ्रीका में चरवाहा जीवन (Pastoralism in Africa – A Comparative Study):
- अफ्रीका में चरवाहों की विशाल आबादी: दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका में रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग सवा दो करोड़ लोग रोजी-रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं।
- पूर्वी अफ्रीका के प्रमुख चरवाहा समुदाय: इनमें बेदुईन्स, बरबेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुरकाना जैसे समुदाय प्रमुख हैं। ये ज्यादातर अर्द्ध-शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ वर्षा आधारित खेती बहुत मुश्किल है। वे गाय-बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ-साथ खेती भी करते हैं।
- औपनिवेशिक काल में अफ्रीका में चरवाहों पर प्रभाव (Impact of Colonialism on African Pastoralists):
- मसाईलैंड का उदाहरण: मसाई चरवाहे पूर्वी अफ्रीका (मुख्यतः केन्या और तंजानिया) में रहते हैं। औपनिवेशिक काल से पहले मसाईलैंड उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया के घास के मैदानों (स्टेपीज़) तक फैला हुआ था।
- भूमि का बँटवारा और चरागाहों का छिन जाना: उन्नीसवीं सदी के आखिर में यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में अपने कब्जे वाली भूमि की सीमाएँ तय कर दीं। 1885 में मसाईलैंड को ब्रिटिश केन्या और जर्मन तांगानिका (बाद में तंजानिया) के बीच बाँट दिया गया।
- इसके बाद, शिकार के लिए आरक्षित क्षेत्र (‘गेम रिजर्व’) बनाए गए (जैसे केन्या का मसाई मारा और साम्बुरु नेशनल पार्क तथा तंजानिया का सेरेनगेटी पार्क) और खेती के लिए श्वेत बस्तियाँ स्थापित की गईं। इन कारणों से मसाई समुदाय अपने लगभग 60 प्रतिशत चरागाहों से हाथ धो बैठा।
- आरक्षित क्षेत्र और आवाजाही पर रोक: औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों को विशेष आरक्षित क्षेत्रों में सीमित कर दिया। इन आरक्षित क्षेत्रों की सीमाएँ भी अक्सर ऐसी जगहों पर तय की गईं जहाँ चारा और पानी की कमी थी। उन्हें इन आरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और उनकी आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए।
- सूखे का प्रभाव और संसाधनों पर बढ़ता दबाव: जब वर्षा नहीं होती थी और चरागाह सूख जाते थे, तो चरवाहों के लिए अपने जानवरों को जीवित रखना मुश्किल हो जाता था। सूखे के वर्षों में मसाई समुदाय के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारी से मर जाते थे। सीमित क्षेत्र में जानवरों की संख्या अधिक होने से चरागाहों पर दबाव और बढ़ गया।
- सरदार और कबीलों पर प्रभाव:
- अंग्रेजों ने कई मसाई उप-समूहों के मुखिया तय कर दिए और उन्हें अपने-अपने कबीले के मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी। इन मुखियों को आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों को लागू करवाने का काम भी दिया गया।
- मुखियों को नियमित रूप से कर इकट्ठा करने और अपने कबीले के लोगों का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई मुखिया समय के साथ अमीर हो गए और गरीब चरवाहों से अलग-थलग पड़ गए।
- मसाई समाज में परंपरागत रूप से ‘एल्डर्स’ (वरिष्ठ जन) और ‘वॉरियर्स’ (योद्धा) के बीच उम्र-आधारित सामाजिक विभाजन था। औपनिवेशिक सरकार ने योद्धाओं की शक्ति को कमजोर किया और उनके द्वारा नियुक्त मुखियों को अधिक महत्व दिया।
- मसाईलैंड का उदाहरण: मसाई चरवाहे पूर्वी अफ्रीका (मुख्यतः केन्या और तंजानिया) में रहते हैं। औपनिवेशिक काल से पहले मसाईलैंड उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया के घास के मैदानों (स्टेपीज़) तक फैला हुआ था।
- बदलावों का सामना करने के तरीके:
- अफ्रीका के चरवाहों ने भी इन बदलावों का सामना करने के लिए जानवरों की संख्या कम की, नए चरागाहों की तलाश की (जहाँ संभव हो सका), और कुछ ने खेती या मजदूरी जैसे अन्य व्यवसायों को अपनाया।
- सीमाएँ बंद हो जाने से उनके व्यापारिक नेटवर्क भी प्रभावित हुए।
- निष्कर्ष: आधुनिक विश्व में चरवाहों का स्थान और भविष्य (Conclusion: Place and Future of Pastoralists in the Modern World):
- आधुनिक विश्व में चरवाहों का जीवन अनेक चुनौतियों से भरा है। चरागाहों का घटना, आवाजाही पर प्रतिबंध, बाज़ारों तक पहुँच की कमी, और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।
- फिर भी, चरवाही आज भी लाखों लोगों के लिए जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण साधन है, खासकर उन शुष्क और पहाड़ी इलाकों में जहाँ खेती संभव नहीं है।
- चरवाहों के पास पर्यावरण और पशुधन प्रबंधन का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है, जिसका महत्व समझने की आवश्यकता है।
- उनके अधिकारों को मान्यता देना, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने के प्रयास आवश्यक हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और पर्यावरण संतुलन में भी योगदान दे सकें।
- कई देशों में अब यह माना जाने लगा है कि घुमंतू चरवाही न केवल पारिस्थितिक रूप से सबसे उपयुक्त तरीका है बल्कि यह शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों के प्रबंधन का एक टिकाऊ तरीका भी हो सकता है।
सहायक सामग्री आधारित अतिरिक्त बिंदु (Points from Supporting Material):
- चरागाहों की गुणवत्ता में गिरावट: जब चरवाहों को निश्चित क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया, तो एक ही भूमि पर बार-बार चराई से चरागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई। उन्हें अपनी प्राकृतिक उर्वरता पुनः प्राप्त करने का मौका नहीं मिला।
- सामाजिक संबंधों में बदलाव: पारंपरिक रूप से, चरवाहों और किसानों के बीच एक सहजीवी संबंध होता था (जैसे धंगर और कोंकण के किसान)। औपनिवेशिक नीतियों ने इन संबंधों को भी प्रभावित किया।
- मसाई समाज में बदलाव: औपनिवेशिक काल में मसाई समाज दो स्तरों पर बँट गया:
- वरिष्ठ जन (एल्डर्स) और योद्धा (वॉरियर्स): परंपरागत सत्ता संरचना।
- मुखिया और आम चरवाहे: औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा बनाई गई नई खाई। अमीर मुखिया शहरों में बस गए, व्यापार करने लगे और अपने गरीब पड़ोसियों की मदद करना छोड़ दिया।
- चरवाहों का लचीलापन: तमाम मुश्किलों के बावजूद, चरवाहा समुदायों ने गजब का लचीलापन दिखाया है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। वे आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- पर्यावरण संरक्षण में भूमिका: कई मामलों में, पारंपरिक चरवाही पद्धतियाँ जैव विविधता और भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं, बशर्ते उन पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए।