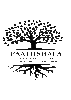अध्याय 2 – संविधान निर्माण
विषय वस्तु
- परिचय: हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?
- संविधान का अर्थ और महत्व।
- विभिन्न प्रकार के शासन और संविधान।
- दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान:
- रंगभेद की नीति और संघर्ष।
- एक नए संविधान की ओर:
- नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC) का संघर्ष।
- रंगभेद शासन का अंत और सुलह की प्रक्रिया।
- सभी के लिए एक साझा संविधान बनाने की चुनौती।
- दक्षिण अफ्रीकी संविधान की मुख्य विशेषताएँ।
- हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? (विस्तृत चर्चा)
- बुनियादी नियमों का समूह जो विश्वास और सहयोग विकसित करे।
- सरकार का गठन कैसे हो और फैसले कौन लेगा, यह स्पष्ट करे।
- सरकार के अधिकारों की सीमा तय करे और नागरिकों के अधिकार बताए।
- अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करे।
- भारतीय संविधान का निर्माण:
- भारत का मार्ग: परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ (विभाजन, रियासतों का विलय, सामाजिक-आर्थिक असमानता)।
- संविधान सभा:
- गठन और चुनाव।
- प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिकाएँ।
- संविधान सभा की कार्यप्रणाली।
- भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य और दर्शन:
- प्रस्तावना (Preamble) का महत्व और उसके मुख्य शब्द (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता)।
- संस्थाओं का स्वरूप: संविधान में विभिन्न संस्थाओं की व्यवस्था।
- निष्कर्ष: संविधान एक जीवंत दस्तावेज़।
विस्तृत नोट्स
- परिचय: हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? (Introduction: Why do we need a Constitution?)
- संविधान का अर्थ (Meaning of Constitution):
- संविधान बुनियादी नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित (या कुछ मामलों में अलिखित) संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है।
- यह सरकार की शक्तियों, उसके गठन, कार्यों और सीमाओं को परिभाषित करता है।
- यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है।
- यह देश का सर्वोच्च कानून होता है और सभी अन्य कानून तथा सरकारी नीतियां संविधान के अनुरूप होनी चाहिए।
- संविधान का महत्व (Importance of Constitution):
- यह विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है।
- यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले लेने का अधिकार किसे होगा।
- यह सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है और नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती।
- यह एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की साझा आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।
- विभिन्न प्रकार के शासन और संविधान (Different types of governance and constitution):
- लगभग सभी देशों का, चाहे वे लोकतांत्रिक हों या न हों, अपना संविधान होता है।
- लोकतांत्रिक देशों में संविधान नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है।
- गैर-लोकतांत्रिक देशों में भी संविधान हो सकता है, लेकिन वह अक्सर शासकों को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है या केवल दिखावटी होता है। असली सवाल यह है कि संविधान कितना प्रभावी है और क्या वास्तव में उसका पालन होता है।
- दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान (Democratic Constitution in South Africa):
दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण यह समझने में मदद करता है कि संविधान क्यों जरूरी है और वह क्या करता है।
- रंगभेद की नीति और संघर्ष (Policy of Apartheid and Struggle):
- दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1994 तक गोरी यूरोपीय अल्पसंख्यक सरकार द्वारा रंगभेद (Apartheid) की नीति लागू की गई थी। यह नस्ली भेदभाव पर आधारित एक अमानवीय व्यवस्था थी।
- लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बाँट दिया गया था: श्वेत (गोरे), अश्वेत (काले), रंगीन (भारतीय मूल के लोग आदि)।
- अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने, उनके साथ घुलने-मिलने, उनके चर्च, अस्पताल, स्कूल, यातायात के साधन इस्तेमाल करने की मनाही थी। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था।
- संगठन बनाने और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करने का भी उन्हें अधिकार नहीं था।
- एक नए संविधान की ओर (Towards a New Constitution):
- नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC): अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC) के झंडे तले अश्वेतों, रंगीन लोगों और कुछ समझदार गोरे लोगों ने रंगभेद की नीति के खिलाफ लंबा और कठिन संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला इस संघर्ष के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्हें रंगभेद का विरोध करने के कारण 1964 से 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था (रॉबेन द्वीप की जेल में)।
- रंगभेद शासन का अंत और सुलह की प्रक्रिया:
- जब विरोध और संघर्ष बहुत बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा, तो गोरी सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- भेदभावपूर्ण कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया और नेल्सन मंडेला को 1990 में आजाद कर दिया गया।
- अंततः 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा फहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्लों के लोगों की मिली-जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला।
- सभी के लिए एक साझा संविधान बनाने की चुनौती:
- रंगभेद समाप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो सभी दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों (गोरे और अश्वेत, दमन करने वाले और दमन सहने वाले) को स्वीकार्य हो।
- दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। अश्वेत बहुसंख्यक यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोकतंत्र में उनके साथ कोई भेदभाव न हो और उन्हें उनके अधिकार मिलें। वे यह भी चाहते थे कि बहुमत के शासन के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता न हो।
- वहीं, गोरे अल्पसंख्यक अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों को लेकर चिंतित थे।
- लंबी बातचीत और समझौतों के बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे की बातों को मानने पर सहमत हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति-एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के आधार पर वे सब कुछ नहीं करेंगे और वे गोरे अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे।
- दक्षिण अफ्रीकी संविधान की मुख्य विशेषताएँ:
- यह संविधान नागरिकों को व्यापक अधिकार देता है, जितने शायद दुनिया के किसी और संविधान ने नहीं दिए हैं।
- इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि इन अधिकारों का उल्लंघन कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।
- इसमें इस बात पर सहमति बनी कि समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, और अतीत के बुरे अनुभवों को भविष्य के इंद्रधनुषी समाज के निर्माण में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।
- दक्षिण अफ्रीकी संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक-दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा भी है – गोरे और काले, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है।
- यह संविधान दुनिया भर के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
- हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? (विस्तृत चर्चा – Why do we need a Constitution? – Detailed Discussion)
दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण हमें बताता है कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
- पहला: बुनियादी नियमों का समूह जो विश्वास और सहयोग विकसित करे (First: A set of basic rules that fosters trust and coordination):
- एक साथ रहने के लिए लोगों के बीच न्यूनतम समन्वय और विश्वास आवश्यक है। यह विश्वास तभी बनता है जब कुछ बुनियादी नियमों पर सहमति हो जिनका पालन सभी करेंगे।
- संविधान ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है जो समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच सहयोग और भरोसे को संभव बनाते हैं।
- दूसरा: सरकार का गठन कैसे हो और फैसले कौन लेगा, यह स्पष्ट करे (Second: To specify how the government will be constituted and who will have power to take which decisions):
- संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी (चुनाव प्रक्रिया, विभिन्न अंगों का गठन आदि)।
- यह भी स्पष्ट करता है कि किस प्रकार के फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन)।
- इससे सरकार के कामकाज में स्पष्टता आती है और मनमानी की गुंजाइश कम होती है।
- तीसरा: सरकार के अधिकारों की सीमा तय करे और नागरिकों के अधिकार बताए (Third: To lay down limits on the powers of the government and tell us what the rights of the citizens are):
- लोकतांत्रिक संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है। ये सीमाएँ इस रूप में होती हैं कि सरकार कुछ विशेष प्रकार के कार्य नहीं कर सकती।
- यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है (जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि) जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। ये अधिकार नागरिकों को सरकार की ज्यादतियों से बचाते हैं।
- चौथा: अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करे (Fourth: To express the aspirations of the people about creating a good society):
- संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह किसी समाज की सामूहिक आकांक्षाओं और मूल्यों का भी प्रतिबिंब होता है।
- यह बताता है कि नागरिक किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं और सरकार को किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए (जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श)।
- भारतीय संविधान का निर्माण (Making of the Indian Constitution):
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था।
- भारत का मार्ग: परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ (The Path to Constitution: Circumstances and Challenges):
- विभाजन की विभीषिका: भारत का संविधान निर्माण एक बहुत ही कठिन दौर में हुआ। देश को धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। यह विभाजन अत्यंत हिंसक और दर्दनाक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और बेघर हुए।
- रियासतों का विलय: आजादी के समय भारत में 500 से अधिक देसी रियासतें थीं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्र रूप से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था। इन रियासतों का भारत में विलय एक बड़ी और जटिल समस्या थी, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से हल किया।
- सामाजिक-आर्थिक असमानता: भारतीय समाज में गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ थीं। गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव जैसी समस्याएँ व्यापक थीं। संविधान निर्माताओं के सामने एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जो इन समस्याओं का समाधान कर सके और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान कर सके।
- भविष्य की चिंता: संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की भी चिंता थी। उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूरा कर सके और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे।
- लोकतांत्रिक अनुभव का लाभ: इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय संविधान निर्माताओं के पास एक बड़ा लाभ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत में भावी संविधान के स्वरूप पर काफी विचार-विमर्श हो चुका था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 1931 के कराची अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा रखी थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी।
- औपनिवेशिक कानूनों से सीख: भारतीय संविधान निर्माताओं ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बने कुछ कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं से भी सीखा, जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act 1935)।
- अन्य देशों के संविधानों से प्रेरणा: उन्होंने दुनिया के अन्य सफल लोकतंत्रों के संविधानों का भी अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा ली (जैसे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिका के मूल अधिकार, आयरलैंड के नीति निदेशक तत्व, फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श)। लेकिन उन्होंने इन विचारों को आँख मूंदकर नकल नहीं किया, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला।
- संविधान सभा (The Constituent Assembly):
- गठन और चुनाव: भारत का संविधान एक ‘संविधान सभा’ द्वारा बनाया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।
- संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसके तुरंत बाद देश दो हिस्सों – भारत और पाकिस्तान में बँट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बँट गई – भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।
- भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे।
- प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिकाएँ: संविधान सभा में भारत के कोने-कोने से आए विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कुछ प्रमुख सदस्य थे:
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद: संविधान सभा के अध्यक्ष।
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष। उन्हें ‘भारतीय संविधान का जनक’ भी कहा जाता है। उन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न जटिल मुद्दों पर गहन चर्चा की।
- सरदार वल्लभभाई पटेल: विभिन्न समितियों के प्रमुख, रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका।
- जवाहरलाल नेहरू: भारत के पहले प्रधानमंत्री, ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ प्रस्तुत किया जिसने संविधान की प्रस्तावना का आधार तैयार किया।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे।
- संविधान सभा की कार्यप्रणाली:
- संविधान सभा ने अत्यंत व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास के साथ काम किया।
- सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और फिर प्रारूप समिति ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया।
- प्रारूप संविधान की प्रत्येक धारा पर कई दौरों में गहन चर्चा हुई। संशोधनों पर विचार किया गया। सदस्यों ने अपने हितों के बजाय देशहित को सर्वोपरि रखा।
- तीन वर्षों (2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन) में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और सँभाला गया है। इन्हें ‘कांस्टीट्यूएंट असेंबली डिबेट्स’ (Constituent Assembly Debates) के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। इन्हीं बहसों से विभिन्न प्रावधानों के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है।
- संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत (Adopt) किया।
- संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू (Enforce) हुआ। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं (26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ‘पूर्ण स्वराज’ का संकल्प लिया था)।
- गठन और चुनाव: भारत का संविधान एक ‘संविधान सभा’ द्वारा बनाया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।
- भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य और दर्शन (Guiding Values and Philosophy of the Indian Constitution):
- भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य और दर्शन उसकी प्रस्तावना (Preamble) में स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। प्रस्तावना पूरे संविधान का सार और उसकी आत्मा है। यह उन आदर्शों को बताती है जिन पर हमारा संविधान और हमारी शासन प्रणाली आधारित है।
- प्रस्तावना के मुख्य शब्द और उनके अर्थ:
- हम भारत के लोग (We, the people of India): यह दर्शाता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और अंतिम संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान किसी बाहरी शक्ति या राजा द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं भारतीय लोगों द्वारा बनाया और अपनाया गया है।
- संप्रभु (Sovereign): भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को निर्देशित नहीं कर सकती।
- समाजवादी (Socialist): (1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) इसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। सरकार लोक कल्याण को बढ़ावा देने और धन एवं संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। हालांकि, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं।
- पंथनिरपेक्ष (Secular): (1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाएगा और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। सरकार धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगी।
- लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic):
- लोकतांत्रिक: सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाएगा और सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। लोगों को अपने शासकों को चुनने और बदलने का अधिकार होगा।
- गणराज्य: राष्ट्र का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।
- न्याय (Justice): सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय: जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
- आर्थिक न्याय: नागरिकों के बीच आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना, सभी को अपनी आजीविका कमाने के समान अवसर।
- राजनीतिक न्याय: सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने, चुनाव लड़ने और सरकारी पदों पर पहुँचने का अधिकार।
- स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है, लेकिन यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- समता (Equality): कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसर की समानता। किसी भी प्रकार के भेदभाव का अंत।
- बंधुता (Fraternity): सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।
- संस्थाओं का स्वरूप (Institutional Design):
- संविधान केवल मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, बल्कि यह इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की एक व्यवस्था भी है।
- भारतीय संविधान सरकार के विभिन्न अंगों – विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary) – की शक्तियों और उनके बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- यह चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की भी व्यवस्था करता है ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है ताकि समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुसार इसमें आवश्यक बदलाव किए जा सकें, लेकिन साथ ही इसके मूल ढांचे को आसानी से बदला न जा सके।
- निष्कर्ष: संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ (Conclusion: The Constitution as a Living Document):
- भारतीय संविधान कोई जड़ या अपरिवर्तनीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज़ है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित और परिवर्तित होता रहता है।
- समाज की बदलती आकांक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।
- न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, ने संविधान की व्याख्या करके इसके अर्थ को और व्यापक बनाया है और इसे समकालीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- संविधान की सफलता केवल उसके प्रावधानों पर ही नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूकता, उनकी सक्रिय भागीदारी और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है।
सहायक सामग्री आधारित अतिरिक्त बिंदु (Points from Supporting Material):
- संविधान सभा की वैधता पर सवाल: कुछ लोग तर्क देते हैं कि संविधान सभा सीधे तौर पर वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, इसलिए यह पूरी तरह से प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। हालांकि, उस समय की परिस्थितियों में यह सबसे व्यवहार्य तरीका था और इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों और विचारों का प्रतिनिधित्व था। इसके अतिरिक्त, संविधान को अपनाने के बाद इसे कभी भी गंभीर चुनौती नहीं मिली, जो इसकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है।
- महात्मा गांधी की भूमिका: हालांकि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों और दर्शन का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर सामाजिक न्याय, ग्राम स्वराज और नैतिक मूल्यों के संबंध में। उन्होंने ‘यंग इंडिया’ पत्रिका में 1931 में ही स्वतंत्र भारत के संविधान से अपनी अपेक्षाएँ व्यक्त की थीं।
- प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर की जगह), टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद)।
- संविधान की भाषा: संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, और इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध कराया गया।
- संविधान की आलोचनाएँ: कुछ आलोचक इसे ‘उधार का थैला’ कहते हैं क्योंकि इसके कई प्रावधान अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं। हालांकि, निर्माताओं ने इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। कुछ इसे अत्यधिक लंबा और वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं।