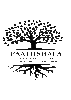अध्याय 1 – कैसे, कब और कहाँ
- इतिहास क्या है? (What is History?)
- इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है।
- यह हमें बताता है कि चीजें अतीत में कैसी थीं और समय के साथ उनमें कैसे बदलाव आए।
- इतिहासकार अतीत को घटनाओं के क्रम में रिकॉर्ड करते हैं।
- तारीखें क्यों महत्वपूर्ण हैं? (Why are Dates Important?)
- इतिहास में तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कौन सी घटना कब हुई।
- पहले, इतिहासकारों को युद्धों और बड़े आयोजनों की तारीखों को याद रखने पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता था।
- लेकिन इतिहास सिर्फ तारीखों का अध्ययन नहीं है। यह इस बारे में भी है कि समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं और विकास करती हैं।
- उदाहरण: लोग कब चाय पीना शुरू किए? यह एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक प्रक्रिया थी।
- कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं? (Which Dates are Important?)
- हर तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती। केवल वे तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं जो किसी विशेष घटना या बदलाव से जुड़ी होती हैं।
- तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम घटनाओं के एक विशेष समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- यदि हम अध्ययन का ध्यान बदलते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं।
- उदाहरण: भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में गवर्नर-जनरल की तारीखें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम भारतीय समाज के इतिहास का अध्ययन करें तो वे कम महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
- हम अवधियाँ (Periods) कैसे निर्धारित करते हैं? (How do we Periodise?)
- इतिहासकार अतीत को बड़े-बड़े कालखंडों या अवधियों में विभाजित करते हैं ताकि अध्ययन को आसान बनाया जा सके।
- यह विभाजन एक विशेष समय में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।
- जेम्स मिल (James Mill) द्वारा कालखंडों का विभाजन:
- 1817 में, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ‘ए हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया’ (A History of British India) नामक एक विशाल पुस्तक लिखी।
- उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन अवधियों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
- उनकी सोच: उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में केवल धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत प्रतिबंध और अंधविश्वास का बोलबाला था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की ओर ले जा सकता है।
- समस्याएँ: मिल का यह विभाजन समस्याग्रस्त था क्योंकि यह भारत के धार्मिक विविधता को नजरअंदाज करता था और यह सुझाव देता था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में कोई प्रगति नहीं थी।
- भारतीय इतिहास का अधिक सामान्य विभाजन:
- आधुनिक भारतीय इतिहासकार आमतौर पर भारतीय इतिहास को प्राचीन (Ancient), मध्यकालीन (Medieval) और आधुनिक (Modern) अवधियों में विभाजित करते हैं।
- आधुनिक काल: इस अवधि को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की शक्तियों के विकास से जुड़ा हुआ माना जाता है।
- समस्याएँ: भारत में, ब्रिटिश शासन के तहत लोगों को समानता, स्वतंत्रता या आर्थिक विकास का अनुभव नहीं हुआ, जिससे कुछ लोग इस अवधि को ‘औपनिवेशिक’ (Colonial) के रूप में संदर्भित करते हैं।
- औपनिवेशिक क्या है? (What is Colonial?)
- जब एक देश दूसरे देश को जीतता है और उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण (Colonisation) कहा जाता है।
- ब्रिटिश शासन के तहत, लोगों को समानता, स्वतंत्रता या आर्थिक विकास नहीं मिला। उन्होंने हमारी फसलों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदला, हमारे रीति-रिवाजों और मूल्यों को बदला।
- इसलिए, इस अवधि को औपनिवेशिक काल कहा जाता है।
- हम इतिहास कैसे जानते हैं? (How do we Know History?)
इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं:
- प्रशासन अभिलेख (Administrative Records):
-
- अंग्रेजों ने हर योजना, निर्णय, समझौता और जांच को लिखना बहुत महत्वपूर्ण माना।
- उनके पास अभिलेखागार (Archives) और अभिलेखागार भवन (Record Rooms) थे जहाँ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र सुरक्षित रखे जाते थे।
- उदाहरण: राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives) और राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum)।
- समस्या: ये अभिलेख हमें केवल आधिकारिक दृष्टिकोण बताते हैं। वे यह नहीं बताते कि आम लोग क्या सोचते थे या वे चीजों को कैसे महसूस करते थे।
- सर्वेक्षण (Surveys):
-
- ब्रिटिश प्रशासन का मानना था कि एक देश पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए, उसे ठीक से जानना होगा।
- उन्होंने कई सर्वेक्षण किए:
- राजस्व सर्वेक्षण (Revenue Surveys): मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पतियों, जीवों, स्थानीय इतिहास और फसलों की जानकारी एकत्र करने के लिए।
- जनगणना (Census): जनसंख्या, जाति, धर्म और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए।
- वानस्पतिक सर्वेक्षण (Botanical Surveys), प्राणीशास्त्रीय सर्वेक्षण (Zoological Surveys), पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Surveys), मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण (Anthropological Surveys), वन सर्वेक्षण (Forest Surveys) आदि।
iii. अन्य स्रोत (Other Sources):
-
- डायरियाँ (Diaries) और आत्मकथाएँ (Autobiographies): लोगों की निजी भावनाएँ और अनुभव।
- यात्रियों के खाते (Accounts of Travellers): उस समय के समाज का वर्णन।
- विभिन्न लोगों द्वारा लिखी गई पुस्तकें: उपन्यास, कविताएँ, आदि।
- समाचार पत्र (Newspapers): सार्वजनिक राय और घटनाओं के बारे में जानकारी।
- कलाकृतियाँ (Artefacts) और स्मारक (Monuments): भौतिक साक्ष्य।