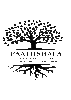अध्याय 2 – भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन
- भूमि संसाधन (Land Resource)
- भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह का केवल लगभग 30% भाग भूमि है, और इस छोटे से प्रतिशत के भी सभी भाग रहने योग्य नहीं हैं।
- जनसंख्या का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है।
- घनी आबादी वाले क्षेत्र: नदियों के मैदान और घाटियाँ (उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता)।
- विरल आबादी वाले क्षेत्र: पहाड़ी इलाके, दलदली भूमि, रेगिस्तान, घने जंगल।
- भूमि उपयोग (Land Use):
- भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे – कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और कारखाने बनाना।
- भूमि का उपयोग भौतिक कारकों (स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता) और मानवीय कारकों (जनसंख्या और प्रौद्योगिकी) द्वारा निर्धारित होता है।
- भूमि का स्वामित्व (Ownership of Land):
- निजी भूमि (Private Land): व्यक्तियों के स्वामित्व में।
- सामुदायिक भूमि (Community Land): समुदाय के स्वामित्व में (जैसे चारागाह, फल, औषधीय जड़ी-बूटी)। इन्हें सांझी संपत्ति संसाधन (Common Property Resources) भी कहते हैं।
- भूमि संसाधन का संरक्षण (Conservation of Land Resource):
- बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती माँगों के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है।
- तरीके: वनरोपण (Afforestation), भूमि पुनः प्राप्त करना (Land Reclamation), रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को विनियमित करना, अतिचारण (Overgrazing) पर नियंत्रण।
- मृदा संसाधन (Soil Resource)
- मृदा पृथ्वी की सतह पर दानेदार पदार्थों की पतली परत है।
- यह भूमि रूप से जुड़ी है।
- मृदा निर्माण (Soil Formation):
- मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने (अपक्षय – weathering) से होता है।
- यह प्रक्रिया लाखों साल लेती है।
- मृदा निर्माण के कारक (Factors of Soil Formation):
- जनक शैल (Parent Rock): मृदा का रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता निर्धारित करता है।
- जलवायु (Climate): तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।
- स्थलाकृति (Topography): ऊँचाई और ढलान मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं।
- समय (Time): मृदा परिच्छेदिका (soil profile) की मोटाई निर्धारित करता है।
- वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव (Flora, Fauna, and Micro-organisms): ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।
- मृदा निम्नीकरण और संरक्षण उपाय (Soil Degradation and Conservation Measures):
- मृदा का निम्नीकरण (खराब होना) और कटाव (Erosion) प्रमुख खतरे हैं।
- कारण: वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा का धोना (Rain wash), भूस्खलन (Landslides), बाढ़।
- संरक्षण के तरीके (Conservation Methods):
- मल्च बनाना (Mulching): पौधों के बीच खाली जमीन को जैविक पदार्थों (जैसे पुआल) की परत से ढकना। यह मृदा की नमी को बनाए रखता है।
- वेदिका फार्म (Terrace Farming): तीव्र ढलानों पर समतल सतहें (सीढ़ियाँ) बनाना ताकि मृदा का कटाव कम हो।
- समुच्चय रेखीय जुताई (Contour Ploughing): पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करना ताकि ढलान से पानी का बहाव धीमा हो।
- रक्षक मेखलाएँ (Shelter Belts): तटीय क्षेत्रों और शुष्क क्षेत्रों में हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाना।
- समोच्च रोधिकाएँ (Contour Barriers): समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास और मिट्टी का उपयोग करके अवरोध बनाना।
- चट्टान बांध (Rock Dam): पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर करना। यह मृदा के कटाव को रोकता है।
- बीच की फसल उगाना (Intercropping): विभिन्न फसलों को एकांतर पंक्तियों में उगाना ताकि बारिश से मिट्टी के धोखे को रोका जा सके।
- जल संसाधन (Water Resource)
- जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है।
- पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग पानी से ढका है। इसलिए इसे जल ग्रह (Water Planet) भी कहते हैं।
- हालाँकि, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का केवल 2.7% ही मीठा पानी (Fresh Water) है।
- इस मीठे पानी का लगभग 70% बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में है, जो दुर्गम हैं।
- इसलिए, मीठे पानी की उपलब्धता बहुत कम है।
- मीठे पानी के स्रोत: नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल (Groundwater)।
- जल की उपलब्धता की समस्याएँ (Problems of Water Availability):
- दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी है।
- यह जलवायु क्षेत्रों में मौसमी या वार्षिक वर्षा में भिन्नता या अति-शोषण के कारण हो सकता है।
- जल संसाधन का संरक्षण (Conservation of Water Resource):
- पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण इसे अनुपयोगी बना सकता है।
- कारण: अपरिष्कृत सीवेज, कृषि रसायन (कीटनाशक, उर्वरक), औद्योगिक कचरा पानी को प्रदूषित करते हैं।
- तरीके:
- वनस्पति आवरण को बनाए रखना (सतही अपवाह को धीमा करने के लिए)।
- औद्योगिक बहिस्रावों (effluents) को बिना उपचारित किए जल निकायों में छोड़ने से रोकना।
- जल संचयन (Rainwater Harvesting) को बढ़ावा देना।
- नहरों को ठीक से अस्तर करना ताकि पानी का रिसाव कम हो।
- खेतों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी कुशल विधियों का उपयोग करना।
- प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन (Natural Vegetation and Wildlife Resource)
- प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल जीवमंडल (Biosphere) में मौजूद होते हैं। जीवमंडल भूमि, जल और वायु का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है।
- पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem): जीवमंडल में सभी सजीव एक-दूसरे पर और अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, जिससे एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।
- उपयोग (Uses):
- वनस्पति: लकड़ी, फल, नट, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज।
- वन्यजीव: दूध, मांस, खाल, ऊन (जानवर), मधुमक्खी परागण (pollination), अपघटन (decomposition)।
- प्राकृतिक वनस्पति का वितरण (Distribution of Natural Vegetation):
- वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है।
- वन (Forests): पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में।
- सदाबहार वन (Evergreen Forests): हमेशा हरे रहते हैं।
- पर्णपाती वन (Deciduous Forests): शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं।
- घास के मैदान (Grasslands): मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में।
- झाड़ियाँ (Shrubs): शुष्क क्षेत्रों में।
- टुंड्रा वनस्पति (Tundra Vegetation): ध्रुवीय क्षेत्रों में काई और लाइकेन।
- प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव का संरक्षण (Conservation of Natural Vegetation and Wildlife):
- वनस्पति और वन्यजीव का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- संकटापन्न प्रजातियाँ (Endangered Species): कई प्रजातियाँ खतरे में हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं (जैसे बाघ)।
- खतरे के कारण: वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल (Forest Fires), सुनामी, भूस्खलन, शिकार (Poaching)।
- संरक्षण के तरीके (Conservation Methods):
- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks), वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserves) स्थापित करना।
- जैव विविधता का संरक्षण: मानव गतिविधियों को विनियमित करना।
- झीलें और आर्द्रभूमि (Wetlands) का संरक्षण: ये महत्वपूर्ण आवास हैं।
- शिकार पर प्रतिबंध लगाना।
- जागरूकता कार्यक्रम: जैसे वन महोत्सव।
- अंतर्राष्ट्रीय समझौते: जैसे CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) जो जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।