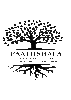अध्याय 3 – ग्रामीण क्षेत्र पर शासन
- कंपनी दीवान बनती है (The Company Becomes the Diwan)
- 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया।
- दीवान के रूप में, कंपनी अब बंगाल प्रांत के मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई।
- कंपनी के उद्देश्य:
- अपनी बढ़ती सेना और व्यापार के खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक राजस्व एकत्र करना।
- भारत में सामान खरीदना और उन्हें इंग्लैंड निर्यात करना।
- राजस्व के लिए संघर्ष (Struggle for Revenue)
- कंपनी ने राजस्व एकत्र करने के लिए एक नियमित प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की।
- समस्या: कंपनी भारत में अच्छी और सस्ती कपास और रेशम खरीदना चाहती थी, लेकिन वे राजस्व से सीधे भुगतान नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए पैसा भारत से ही आए।
- बंगाल में अकाल (Famine in Bengal – 1770):
- बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में थी।
- 1770 के अकाल ने बंगाल की एक-तिहाई जनसंख्या को मार डाला, जिससे उत्पादन और राजस्व में और कमी आई।
- इस अकाल ने ब्रिटिश अधिकारियों को एहसास कराया कि कृषि में निवेश और राजस्व प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
- कृषि में सुधार की आवश्यकता (Need to Improve Agriculture)
- कंपनी ने महसूस किया कि अगर वे कृषि में सुधार नहीं करते हैं, तो राजस्व आय में गिरावट आएगी।
- स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement – 1793):
- लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis) द्वारा पेश किया गया।
- उद्देश्य: राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना और जमींदारों को भूमि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- नियम:
- राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों (Zamindars) के रूप में मान्यता दी गई।
- उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार दिया गया।
- राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी।
- स्थायी बंदोबस्त की समस्याएँ (Problems with Permanent Settlement):
- जमींदारों के लिए: राजस्व बहुत अधिक तय किया गया था, इसलिए कई जमींदार भुगतान करने में विफल रहे और उनकी जमींदारी छीन ली गई।
- किसानों के लिए: जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार किया और उनकी जमीन छीन ली। किसान ऋणग्रस्त होते गए।
- एक नई व्यवस्था: महलवाड़ी बंदोबस्त (A New System: The Mahalwari Settlement)
- 19वीं सदी की शुरुआत में, कंपनी को और अधिक पैसे की आवश्यकता थी।
- हॉल्ट मैकेंजी (Holt Mackenzie) द्वारा 1822 में पेश किया गया।
- क्षेत्र: उत्तर-पश्चिमी प्रांत (उत्तरी भारत का हिस्सा)।
- नियम:
- राजस्व व्यक्तिगत किसानों से नहीं, बल्कि गाँव (महल) से एकत्र किया जाना था।
- प्रत्येक गाँव या महल का अनुमानित राजस्व निकाला गया और प्रत्येक महल को एक या एक से अधिक गाँवों का समूह माना गया।
- राजस्व को समय-समय पर संशोधित (revise) किया जा सकता था, यह स्थायी नहीं था।
- गाँव के मुखिया (Headman) को राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का काम सौंपा गया।
- मुनरो व्यवस्था या रैयतवाड़ी (The Munro System or Ryotwari)
- दक्षिण भारत में, ब्रिटिश अधिकारियों ने महसूस किया कि वहाँ कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे।
- कैप्टन अलेक्जेंडर रीड (Captain Alexander Read) ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अधिग्रहित कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया।
- थॉमस मुनरो (Thomas Munro) ने इसे व्यापक रूप से विकसित किया।
- क्षेत्र: दक्षिण भारत।
- नियम:
- राजस्व सीधे रैयतों (Ryots) यानी किसानों से एकत्र किया जाता था।
- उनकी भूमि का सर्वेक्षण किया गया और राजस्व सीधे उनके साथ तय किया गया।
- मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पितृसत्तात्मक पिता की तरह काम करना चाहिए और किसानों की रक्षा करनी चाहिए।
- समस्याएँ:
- राजस्व की दर बहुत अधिक थी।
- किसान अपनी जमीन छोड़कर भागने लगे, जिससे गाँव वीरान हो गए।
- यूरोप के लिए फसलें (Crops for Europe)
- 18वीं सदी के अंत तक, कंपनी ने महसूस किया कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र न केवल राजस्व प्रदान कर सकता है बल्कि यूरोप के लिए आवश्यक फसलों का उत्पादन भी कर सकता है।
- कंपनी ने किसानों को अफीम (Opium) और नील (Indigo) जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया।
- नील की खेती (Indigo Cultivation):
- यूरोप में नील की माँग: नील का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। 18वीं सदी तक भारतीय नील की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत माँग थी।
- नील की खेती के प्रकार (Two Main Systems of Indigo Cultivation):
- निज (Nij) खेती: बागान मालिक सीधे अपनी जमीन पर खेती करते थे (या तो मजदूरों को लगाकर या किराए पर जमीन लेकर)। यह बड़ी समस्या थी क्योंकि इसमें बहुत अधिक श्रमिकों और हल-बैलों की आवश्यकता होती थी।
- रैयती (Ryoti) खेती: बागान मालिक रैयतों (किसानों) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे।
- रैयतों को कम ब्याज पर ऋण मिलता था।
- रैयत अपनी कम से कम 25% भूमि पर नील उगाते थे।
- फसल काटने के बाद, बागान मालिक उन्हें कम कीमत पर खरीदते थे।
- समस्याएँ: नील को अच्छी उपजाऊ भूमि पर उगाया जाता था, जहाँ किसान चावल उगाना चाहते थे। नील की जड़ें मिट्टी को थका देती थीं, जिससे चावल की खेती मुश्किल हो जाती थी। कीमतें बहुत कम थीं।
- नील विद्रोह (Blue Rebellion – March 1859):
- बंगाल के हजारों रैयतों ने नील उगाने से इनकार कर दिया।
- उन्होंने बागान मालिकों का विरोध किया, लाठियों और तलवारों से हमला किया।
- उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे बागान मालिकों से ऋण नहीं लेंगे और नील की खेती नहीं करेंगे।
- ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग (Indigo Commission) का गठन किया जिसने बागान मालिकों को दोषी ठहराया और रैयतों को नील की खेती न करने की अनुमति दी।
- इसके बाद, नील का उत्पादन बंगाल से बिहार में स्थानांतरित हो गया।