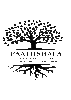अध्याय 4 – न्यायपालिका
- न्यायपालिका की भूमिका क्या है? (What is the Role of the Judiciary?)
- न्यायपालिका (Judiciary) सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करने और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- यह अदालतों की एक प्रणाली है।
- न्यायपालिका के मुख्य कार्य:
- विवाद समाधान (Dispute Resolution):
-
-
- न्यायपालिका नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो राज्य सरकारों के बीच, और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करती है।
- उदाहरण: संपत्ति विवाद, तलाक के मामले, आपराधिक मामले।
-
- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review):
-
-
- न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति है।
- यदि न्यायपालिका को लगता है कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह उसे रद्द (strike down) कर सकती है।
-
iii. कानून का शासन बनाए रखना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना (Upholding the Law and Enforcing Fundamental Rights):
-
-
- न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हों।
- यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की रक्षा करती है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत जा सकता है।
-
- स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? (What is an Independent Judiciary?)
- स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) का अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) के नियंत्रण में नहीं होती।
- इसका मतलब है कि न्यायाधीश अपनी भूमिका निभाते समय स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सरकार से प्रभावित नहीं होते।
- स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह सुनिश्चित करती है कि कानून का शासन (Rule of Law) बना रहे।
- यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है।
- यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
- स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है?
- न्यायाधीशों की नियुक्ति: न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है।
- न्यायाधीशों को हटाना: न्यायाधीशों को हटाना बहुत मुश्किल होता है (केवल महाभियोग – impeachment द्वारा)।
- वेतन और भत्ते: न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय नहीं किए जाते हैं।
- भारत में न्यायालयों की संरचना (Structure of Courts in India)
भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System) है, जिसका अर्थ है कि अदालतों का एक
पिरामिड जैसा ढाँचा है।
- सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court):
-
- यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है।
- यह नई दिल्ली में स्थित है।
- इसके निर्णय भारत के सभी अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।
- उच्च न्यायालय (High Courts):
-
- ये राज्यों में शीर्ष अदालतें हैं।
- प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है (या दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय)।
- ये अपने संबंधित राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों (subordinate courts) के निर्णयों की समीक्षा करते हैं।
iii. जिला न्यायालय / अधीनस्थ न्यायालय (District Courts / Subordinate Courts):
-
- ये प्रत्येक जिले में या शहर में स्थापित होते हैं।
- इनमें विभिन्न प्रकार के न्यायालय शामिल होते हैं, जैसे:
- दीवानी न्यायालय (Civil Courts): संपत्ति, अनुबंध आदि से संबंधित मामले।
- फौजदारी न्यायालय (Criminal Courts): चोरी, हत्या आदि से संबंधित मामले।
- ये अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय देते हैं।
- न्याय तक पहुंच (Access to Justice)
- भारत के सभी नागरिक अदालतों तक पहुँच सकते हैं।
- हालाँकि, गरीबों के लिए अदालत जाना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है।
- जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL):
- 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था विकसित की।
- यह किसी भी व्यक्ति या संगठन को सार्वजनिक हित में मुकदमा दायर करने की अनुमति देती है, भले ही वे सीधे तौर पर प्रभावित न हों।
- इससे गरीबों और वंचितों को न्याय तक पहुँचने में मदद मिली है।
- उदाहरण: बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाना।
- क्या हर कोई अदालत जा सकता है? (Can Everyone Access the Courts?)
- सिद्धांत रूप में, हाँ, सभी नागरिक अदालत जा सकते हैं।
- लेकिन व्यवहार में, अदालतों में प्रक्रियाएँ लंबी, महंगी और जटिल हो सकती हैं, जो विशेष रूप से गरीबों के लिए एक चुनौती है।
- यही कारण है कि PIL जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि न्याय तक पहुँच को आसान बनाया जा सके।